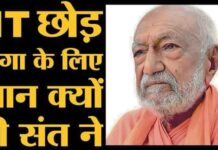— नंदकिशोर आचार्य —
संस्कृति की चर्चा में इस बात की अनदेखी की जाती रही है कि हम अधिकांशतः संस्कृति के नाम पर उन उपकरणों की चर्चा ही करते रह जाते हैं जिनके माध्यम से उसके बाह्य स्वरूप की भी औपचारिक पहचान ही हो पाती है और मूल तत्त्व अक्सर अनछुआ ही रह जाता है। उस मूल तत्त्व की खोज और फिर उसके सहारे सांस्कृतिक उपकरणों की बनावट की पहचान अर्थात् तात्त्विक और अभिव्यक्त स्तर पर संस्कृति के मूल आधार का ज्ञान ही संस्कृति का वास्तविक ज्ञान है- बाकी सारी चर्चा तो वही है जिसे अँगरेजी मुहावरे में ‘बीटिंग अबाउट बुश’ कहा जाता है। यही कारण है कि आधुनिक कहा जाने वाला समाज अधिकांशतः संस्कृति को एक ऐतिहासिक वस्तु मानता है- और आश्चर्य नहीं कि इसीलिए विश्वविद्यालयों में ‘प्राचीन इतिहास और संस्कृति’ के विभाग एक ही होते हैं और क्योंकि इतिहास कभी वर्तमान नहीं होता अतः वर्तमान संस्कृति का कोई विभाग भी क्यों हो!– और इसीलिए संस्कृति आधुनिक समाज के लिए सजावट का सामान हो जाती है।
कुछ अन्य लोग होते हैं- और वे पहले वर्ग से तो कुछ बेहतर ही होते हैं- जो संस्कृति को एक जीवित वस्तु तो मानते हैं पर उनका तात्पर्य एवं संबंध कला-साहित्य आदि के प्रति एक उदार संरक्षक भाव से ही अधिक होता है। उनकी समझ में यह आना मुश्किल होता है कि यदि किसी समाज में कला और साहित्य को पर्याप्त आर्थिक संरक्षण प्राप्त है लेकिन अपने व्यापक आचरण में वह समाज एक शोषक, आततायी और हिंसक समाज है तो उसे सांस्कृतिक दृष्टि से भी अविकसित क्योंकर कहा जा सकता है जबकि कला और साहित्य को वहाँ श्लाघनीय सुविधाएँ और सम्मान प्राप्त हैं।
इस वर्ग के लोगों की नजर में तो कला और साहित्य को पुरस्कृत करने वाला वह व्यक्ति भी एक सांस्कृतिक व्यक्ति है जिसकी सारी संपन्नता अपने से इतर के शोषण और दमन पर टिकी है। यही कारण है कि इतिहास में दो-चार इमारतें बनवा देने या किसी लेखक-विद्वान को अपने दरबार में आश्रय दे देने के कारण ऐसे धर्मान्ध और अत्याचारी शासकों और अन्य व्यक्तियों को भी संस्कृति का संरक्षक कहा गया है जिनके अन्य सारे कार्यों को निन्दनीय और मानवविरोधी ही कहा जाएगा।
जाहिर है कि कला और साहित्य, सांस्कृतिक चेतना की अभिव्यक्ति के उपकरण हैं और उपकरणों का सम्मान तब तक संस्कृति का सम्मान नहीं माना जा सकता जब तक कला और साहित्य में अभिव्यक्त हो रही मूल्यचेतना का भी व्यावहारिक स्तर पर सम्मान न हो। इसके बिना भी यदि समाज में कला या साहित्य के प्रति सम्मान का भाव प्रदर्शित किया जाता है- जैसा कि आजकल बहुधा किया जाता है- तो यही मानना होगा कि वह समाज एक सांस्कृतिक पाखंड का शिकार है।
स्पष्ट है कि संस्कृति का आधार किसी समाज का मूल्य-बोध और उसकी कसौटी उस समाज का आचरण है। यदि ऐसा है तो संस्कृति की चर्चा में हम उसे सदैव कालबद्ध या देशबद्ध कर क्यों देखते हैं?
अध्ययन की सुविधा के लिए हम यदि उसका वर्गीकरण करें भी तो उसे आत्यंतिक नहीं बना दिया जाना चाहिए जबकि होता यही है कि हम उसे न केवल अलग-अलग खाँचों में बाँट देते हैं बल्कि इस विभाजन को ही वास्तविक संस्कृति मान लेते हैं और अन्य खाँचों से उसकी एकसूत्रता बनाने की बजाय उसका अलगाव बताने और इसे बनाये रखने में ही सारी शक्ति-श्रम व्यय करते हैं।
मेरे मन को यह बात निरंतर मथती रही है कि यदि संस्कृति मूल्य-दृष्टि है तो वह सार्वभौम है- और तब उसे देश-प्रदेश की सीमाओं में बाँट कर देखना बुनियादी रूप से गलत है।
यदि संस्कृति एक मूल्यगत प्रक्रिया है तो वह एक सार्वभौम और सनातन प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया का बुनियादी प्रयोजन और लक्ष्य एक ही है, उसकी मूल प्रवृत्ति और आकांक्षा एक ही होनी चाहिए। यदि उसके बाह्य स्वरूप में कोई परिवर्तन दिखाई भी देते हैं तो वे संदर्भगत परिवर्तन हैं जिनसे मूल आधार पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। ऐसी स्थिति में संस्कृति के देशबद्ध रूप पर अधिक जोर देना या उसी को किसी के लिए अनिवार्य मान लेना क्या प्रकारांतर से संस्कृति की मूल अवधारणा का ही विरोध करना नहीं है?
कुछ लोग कह सकते हैं कि देशकाल के अनुसार मूल्य बदलते रहते हैं, अतः विभिन्न देश-प्रदेशों की संस्कृति यदि एक-दूसरे से अलग है तो अलगाव स्वाभाविक है। लेकिन ऐसा कहने वाले यह भूल जाते हैं कि समय और संदर्भ के अनुसार मूल्यों के स्वरूप में तो परिवर्तन हो सकता है, होता है लेकिन मूल्यों की मूल प्रकृति नहीं बदलती। भौगोलिक और पर्यावरण के कारणों से मनुष्यगत अनिवार्यताओं के कारण कुछ परिवर्तन होते भी हैं तो उन्हें आत्यंतिक मान लेना क्या एक प्रकार का दुराग्रह ही नहीं है?
मध्यकाल तक तो संस्कृति की देशबद्ध धारणा का कुछ आधार फिर भी हो सकता था। जब तक संस्कृति या मूल्य-चेतना का मुख्य आधार जाति या धर्म रहा तब तक विभिन्न धर्मव्यवस्थाओं को मानने वाले देशों और विभिन्न जातियों में यदि कुछ मूलभूत अंतर दिखाई भी दिये तो यह अस्वाभाविक नहीं था। लेकिन आज जब विभिन्न जातियाँ आपस में घुलमिल चुकी हैं तथा अलग से उनकी पहचान कर पाना संभव नहीं रह गया है और धर्म का- खासतौर से उपासना पद्धति का- जीवन और व्यवस्था पर वैसा नियंत्रण और केंद्रीय प्रभाव नहीं रह गया है जो प्राचीन और मध्ययुग तक था तो संस्कृति को देशबद्ध रूप में देखने या विकसित करने की क्या सार्थकता हो सकती है?
विभिन्न धर्मों के विश्वासों और आचार में कुछ बुनियादी एकता थी तो कुछ बुनियादी भिन्नताएँ भी थीं और इसलिए उनके आधार पर विकसित मूल्यों में कुछ भिन्नताएँ हो सकती थीं जिससे किसी धर्मविशेष के अनुयायी समाज या क्षेत्र के लिए एक भिन्न संस्कृति का विकास संभव था। लेकिन आधुनिक समाज में धर्म प्रभुतासंपन्न स्थान खोता जा रहा है और धर्म के रूढ़िगत स्वरूप और विश्वासों को मानव अपने विवेक की कसौटी पर कसने लगा है। दूसरे शब्दों में, इसका तात्पर्य यह हुआ कि मूल्य-दृष्टि को निर्देशित करने वाला तत्त्व अब शास्त्र या धर्म नहीं बल्कि मनुष्य का अपना विवेक हो गया है। यह विवेक सार्वभौम है, किसी भौगोलिक सीमा या राजनीतिक नागरिकता से संबद्ध नहीं। ऐसी स्थिति में एक सनातन प्रक्रिया के रूप में संस्कृति की देशबद्धता की आत्यंतिकता का आग्रह क्या दुराग्रह, या कुछ उदार होकर सोचें तो पूर्वग्रह नहीं है?
आपत्ति उठायी जा सकती है कि धर्म अभी भी केन्द्रीय प्रेरक तत्त्व बना रह सकता है, कि विज्ञान धर्म को कभी भी पूर्णतया पदच्युत नहीं कर सका, कि विज्ञान भी धर्म की बहुत-सी बातों को स्वीकार करता जा रहा है, कि अब धर्म कोई संप्रदाय नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है और उसी के आधार पर भावी संस्कृति का विकास होगा आदि-आदि। लेकिन इन सभी आपत्तियों को सही मान लेने पर भी संस्कृति की देशबद्धता की अनिवार्यता पर तो प्रश्नचिह्न लगा ही रहता है- और तब क्या देश भी एक सांस्कृतिक स्वाभाविकता से अधिक एक भौगोलिक अनिवार्यता और राजनैतिक आवश्यकता ही नहीं रह जाता?
संस्कृति को अक्सर किसी भाषा या धर्म-संप्रदाय या देश के साथ जोड़कर देखा जाता रहा है- यथा बंगला संस्कृति, हिन्दू संस्कृति, मुस्लिम संस्कृति, ईसाई संस्कृति, भारतीय संस्कृति, फ्रेंच संस्कृति आदि। लेकिन ऐसा विभाजन यदि एक मूलभूत संस्कृति के संदर्भगत और परिवेशगत विभिन्न स्वरूपों को समझने के लिए किया जाय तो कुछ सीमा तक उसकी अपनी उपादेयता भी है लेकिन इस विभाजन को आत्यंतिक मानकर इसे ही विभिन्न समाजों या व्यक्तियों के सांस्कृतिक आचरण की एकमात्र कसौटी बना लेना क्या एक सांस्कृतिक पाखंड को विकसित होने देना नहीं है?
किसी जमाने में संस्कृति की चर्चा अधिकांशतः धर्म के साथ जोड़कर की जाती थी। फिर यह चर्चा राष्ट्र के साथ जोड़ कर की जाने लगी। अब लगता है कि यदि संस्कृति की बात पूरी मानव जाति के संदर्भ में नहीं की जाती है और हमारा ध्यान स्वरूपगत भिन्नताओं के कारण अलगाव को पुष्ट करते रहने की बजाय प्रकृतिगत बुनियादी एकता को पुष्ट करने की ओर नहीं जाता है तो यह सांस्कृतिक विकास की प्रक्रिया में एक ऐतिहासिक विसंगति की ओर से आँखें मूँदना होगा जिसके परिणाम पूरी मानव जाति को, और इसलिए हमें भी, भुगतने होंगे।
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.