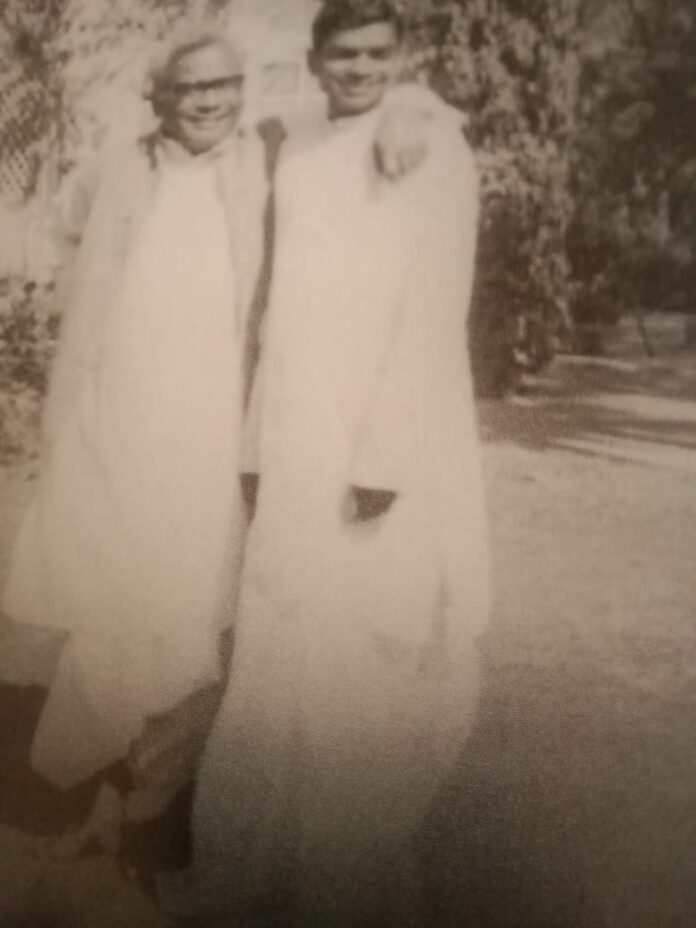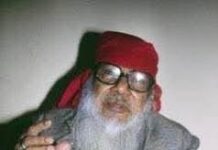— किशन पटनायक —
सोशलिस्ट पार्टी 1958 तक काफी टूट चुकी थी। ‘मैनकाइंड’ में जो लोग काम करते थे, वे छोड़कर जाने वाले थे। हठात लोहिया से मुझे खबर मिली कि मैं कलकत्ता में जाकर उनसे मिलूँ। ले कलकत्ता बीच-बीच में आकर रहते थे। मैं समझ नहीं सका क्यों बुलाया है। इसके पहले लोहिया के साथ कभी कोई बातचीत नहीं हुई थी।
मैनकाइंड निकलने के बाद मैंने एक या दो छोटे लेख भेजे थे। संपादक को लिखे जाने वाले पत्रों की शैली में। शायद इसी से उन्होंने सोचा होगा कि पत्रिका की जिम्मेवारी सँभाल लूँगा।
भेंट होने पर उन्होंने कहा कि तुम्हें हैदराबाद जाना होगा। तब मैनकाइंड का स्तर मुझे बहुत ऊँचा लगता था। यह 1959 की बात है। मैनकाइंड के लिए हेक्टर अभयवर्धन सचमुच एक पूरी तरह से उपयुक्त आदमी थे। अगर पहले से ही मुझे पता होता कि वे मैनकाइंड छोड़ जा रहे हैं और इसलिए मुझे बुलाया गया तो मैं जरूर आपत्ति करता, लेकिन लोहिया ने मुझे कुछ बताया नहीं और कहा कि तुम हैदराबाद जाओ और वहाँ ज्वायन करो। मैं राजी हो गया।
पर वहाँ जाने पर देखा कि हेक्टर अभयवर्धन और उनके साथ के लोग मैनकाइंड छोड़ने के लिए तैयार बैठे थे, बस मेरे पहुँचने पर उन्हें चले जाना था। उन्होंने सब पहले से ही लोहिया को बता दिया था कि वे और काम नहीं करेंगे। तब मेरी आयु तीस वर्ष से भी कम थी। हेक्टर अभय वर्धन पचास के आसपास के होंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इन लोगों के चले जाने पर मैं काम कैसे सँभाल पाऊँगा। जो भी हो, मेरे वहाँ पहुँचने के पंद्रह-बीस दिन के बाद वे लोग चले गये। मुझे काफी असुविधा महसूस हुई। अब क्या होगा, क्या करूँगा।
मैनकाइंड निकलने के पीछे एक कारण था। भारत में स्वाधीनता के समय से एक वैश्विक ग्रुप था जो कम्युनिस्ट था पर स्टालिन का विरोधी। अन्यथा यह ग्रुप पूरी तरह मार्क्सवादी-लेनिनवादी था। वह जो ग्रुप था वह लोहिया के साथ मिल गया। ग्रुप के भीतर काफी सक्रिय लोग नहीं थे। केवल मद्रास से एक ट्रेड यूनियन के कुछ लोग थे, उनके नाम भूल रहा हूँ। मुख्य व्यक्ति थे हेक्टर अभयवर्धन, वे बौद्धिक नेता थे। एक हिसाब से वे मार्क्सवादी पंडित व्यक्ति थे। अन्य कोई क्रियाकलाप न होने पर भी वे बौद्धिक रूप से सक्रिय थे। वे हैदराबाद आ गये। वे ही मुख्यतया मैनकाइंड के कार्यकरारी संपादक थे। उनका नाम भी संपादक मंडल में जाता था। उनके कारण ही पत्रिका सुचारु रूप से प्रकाशित होने लगी। वे संपादन का काम गंभीरता से करते थे। स्थानीय लोगों ने दल नहीं छोड़ा था, सहायता की।
दूसरी बात यह हुई कि विजयनगरम के राजा ने भी छोड़ दिया था। बदरीविशाल पित्ती को अधिक आर्थिक सहायता करनी पड़ती थी। वे मैनकाइंड में जितना पैसा लगाते थे, उसे कम करना चाहते थे क्योंकि उनको दूसरे खर्च भी वहन करने पड़ते थे। मैनकाइंड के लिए जिस कागज का उपयोग किया जाता था वे उसकी जगह कम पैसे के कागज का उपयोग करने लगे। मुझे लगा कि मेरे यहाँ आने पर यह सोचा जाएगा कि मैनकाइंड का कलेवर पहले जैसा नहीं है, उसका स्तर गिर गया है। जो भी हो, मुझे काम करना ही था।
लोहिया जी पहले संपादकीय नहीं लिखते थे। यह मैनकाइंड की एक शैली थी। प्रथम अंक से यह होता आया था कि लेख जितना लंबा होता, संपादकीय भी उतना लंबा होता। लेख छोटा करके मैंने लिखने का प्रयत्न किया। फिर मैंने लोहिया को चिट्ठी लिखी कि मुझे पता नहीं था कि जो लोग पहले से काम करते थे वे सभी चले जाएँगे। आपने कैसे सोच लिया कि मैं इसे सँभाल पाऊँगा? मेरी तो इतनी क्षमता नहीं है। फिर मैं संपादकीय कैसे लिखूँ? लोग जो पहले का संपादकीय पढ़ चुके हैं, उन्हें अबका संपादकीय अच्छा नहीं लगेगा।
लेकिन लोहिया ने मेरे पत्र का जवाब नहीं दिया। दो-तीन अंक में संपादकीय छपने के बाद लोहिया ने अपने एक महिला मित्र की एक चिट्ठी को मेरे पास भेज दिया। वह महिला मित्र, उन दिनों दिल्ली में प्रोफेसर थीं, वे लंदन गयी हुई थीं। उन्होंने लोहिया को लंदन से ही चिट्ठी लिखी कि इस बार आपने जो संपादकीय लिखा है, गजब है। लोहिया ने उनकी उसी चिट्ठी को मेरे पास भेज दिया। इससे संपादकीय लिखने के प्रति मेरा आत्मविश्वास बढ़ा।
धीरे-धीरे सब लोगों के छोड़कर चले जाने के बाद रुपए-पैसे की असुविधा होने लगी। सरकुलेशन पहले से कम हो गया। इस प्रकार यह अवनति की राह पर चलन लगा।
(किशन जी का यह संस्मरण अशोक सेकसरिया और संजय भारती द्वारा संपादित किताब ‘किशन पटनायक : आत्म और कथ्य’ से लिया गया है; किताब कोलकाता के रोशनाई प्रकाशन ने छापी है।)
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.