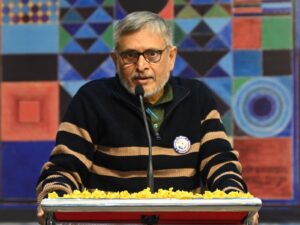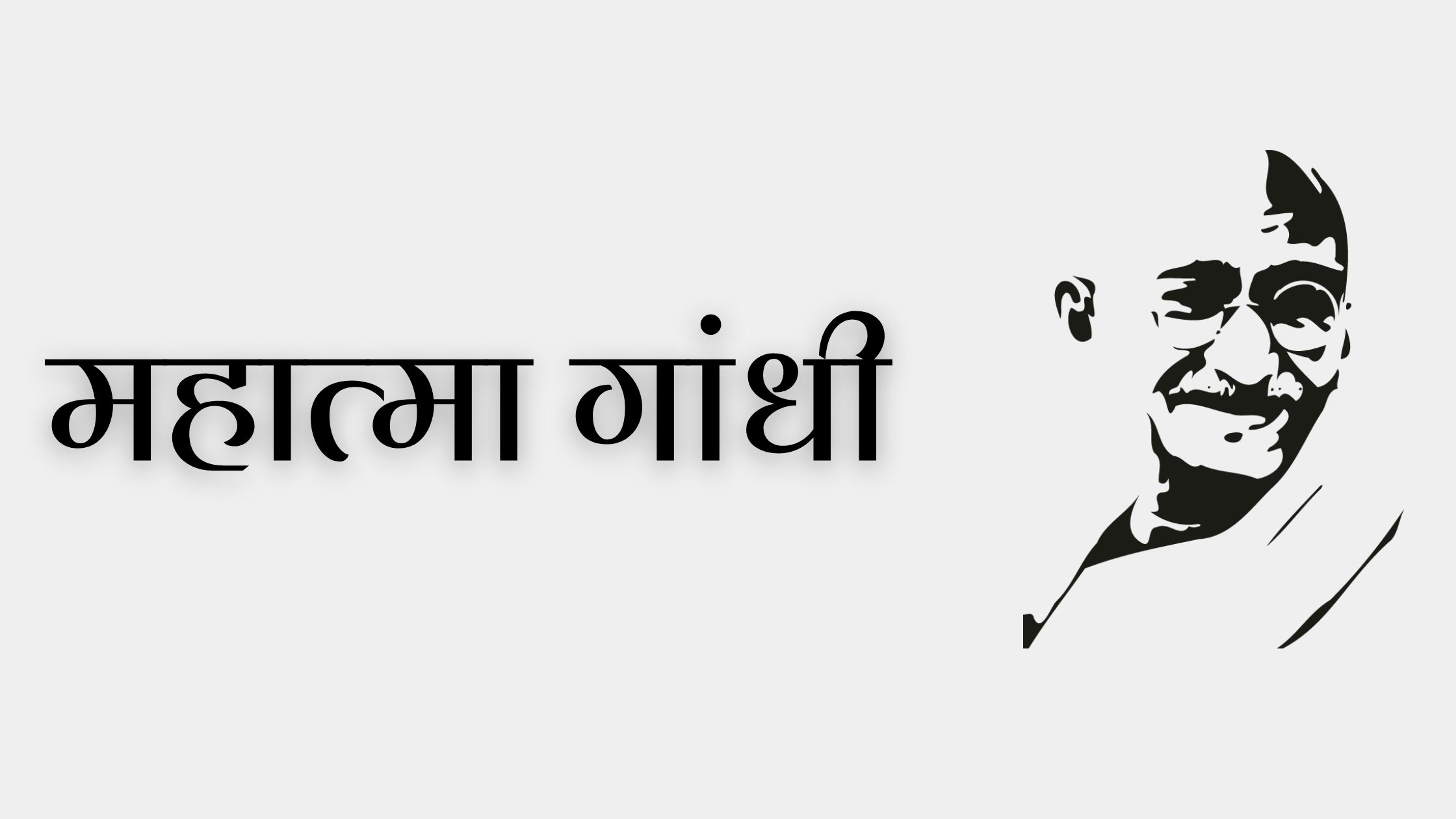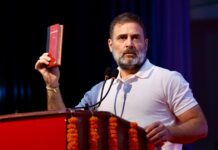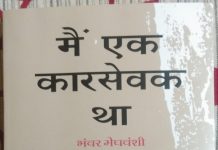— अरुण कुमार त्रिपाठी —
आदरणीय मंच और सभागार में उपस्थित सज्जनों। गांधी और डा आंबेडकर में सामंजस्य कराने के लिए मैं पिछले 35 सालों से सक्रिय हूं। इस विषय पर नवभारत टाइम्स जैसे देश के प्रमुख अखबार में सन 1990 में मेरा पहला लेख काफी चर्चित रहा था।उसका शीर्षक था गांधी को आंबेडकर से न लड़ाएं।
इसमें कोई दो राय नहीं कि गांधी और आंबेडकर के बीच मतभेद और विवाद थे। लेकिन वे मतभेद साधन को लेकर थे। न कि साध्य को लेकर। भारतीय समाज में समता और समृद्धि आए। नागरिकों को स्वतंत्रता हासिल हो, और एक नैतिक और अहिंसक समाज बने इस मायने में दोनों महापुरुषों में कोई मतभेद नहीं था। सबसे बड़ी बात है वह है बंधुता, प्रेम और मैत्री की।इस मोर्चे पर गांधी और आंबेडकर में अद्भुत समानता है।
जहां तक संविधान की बात है तो वह आधुनिक राष्ट्र के लिए उसके नागरिकों द्वारा बनाया जाने वाला ऐसा धर्मग्रंथ है जिससे प्रेरणा और निर्देश लेकर नागरिक और राज्य की संस्थाएं अपने दैनंदिन जीवन को संचालित करते हैं और भावी जीवन की योजनाएं बनाते हैं। लेकिन यह आधुनिक धर्मग्रंथ प्राचीन धर्मग्रंथों से इस मायने में अलग है क्योंकि इसकी रचना न तो इलहाम से होती है और न ही यह ईश्वर की वाणी से अवतरित होता है। इसीलिए इसमें संशोधन किया जा सकता है।
जहां तक संविधान से या संविधान निर्माण से गांधी और आंबेडकर का संबंध है तो हमें इस ऐतिहासिक तथ्य को नहीं भूलना चाहिए कि हमारा संविधान पर औपनिवेशिक प्रभाव के बावजूद इस पर स्वतंत्रता आंदोलन यानी महात्मा गांधी का असर है तो साथ ही साथ डा आंबेडकर के सामाजिक न्याय आंदोलन का भी गहरा असर है। एक बात जरूर कही जा सकती है कि हमारी संविधान सभा में प्राचीन भारतीय के गणतंत्रीय मॉडलपर आधारित यानी गांधी के विचारों के अनुसार एक विकेंद्रित संविधान बनाने की चर्चा है लेकिन व्यावहारिक तौर पर यह यूरोप और अमेरिका के संविधानवादी दर्शन के अनुसार ही निर्मित किया गया। यानी इसके व्यावहारिक पक्ष पर डा आंबेडकर के विचार दर्शन का प्रभाव ज्यादा है।
महात्मा गांधी तो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे लेकिन उनके अनुयायी संविधान सभा से लेकर उसके बाहर तक यह प्रयास कर रहे थे कि संविधान का स्वरूप ग्राम पंचायतों पर आधारित हो और विधानसभाओं और पार्लियामेंट के लिए प्रत्यक्ष चुनाव न होकर परोक्ष चुनाव हो।
दूसरी ओर डा आंबेडकर का संविधान सभा में चयन काफी उथल पुथल भरा है। वे पहली बार दिसंबर 1946 में बंगाल से संविधान सभा के लिए चुने गए। उस समय मुस्लिम लीग ने उनकी मदद की थी। इसमें उनके मित्र और बाद में पाकिस्तान के कानून मंत्री बने जोगेंद्र नाथ मंडल की बड़ी भूमिका थी। मंडल भी संविधान विशेषज्ञ थे और पाकिस्तान के दलितों के हित के लिए वहां संविधान बनाने गए लेकिन बुरी तरह विफल होकर भारत लौट आए। डॉ आंबेडकर की कहानी उसके ठीक विपरीत है।
लेकिन इस पूरी कहानी को सुनने और जानने से पहले हमें यह नहीं भूलना चाहिए आजादी से पहले स्वयं भारतीय उपमहाद्वीप भी भारी उथल पुथल से गुजर रहा था। जब हमारी आजादी और संविधान निर्माण का समय आया तो देश का विभाजन हो गया और चारों ओर मारकाट मच गई थी। मारकाट तो 1946 से ही शुरू हो गई थी। मुस्लिम लीग और उसके नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 कोडायरेक्ट एक्शन डे यानी सीधी कार्रवाई की घोषणा की थी और उसके चलते दंगे और भारी हिंसा हुई थी। गांधी उन दंगों को शांत करने निकल पड़े थे। अगर आंबेडकर भारतीय संविधान निर्माण में जुटने की अपनी तैयारी कर रहे थे तो महात्मा गांधी इस महाद्वीप को शांत करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहे थे।
लेकिन जब 15 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के साथ बंगाल का एक हिस्सा पाकिस्तान चला गया तो डा आंबेडकर की संविधान सभा की सदस्यता चली गई। इस दौरान उनको फिर से संविधान सभा में लिए जाए जाने के बारे में तमाम कहानियां हैं। एक कहानी तो यह है कि गांधी और नेहरू ने साजिश करके डॉ आंबेडकर को संविधान सभा से निकलवा दिया। वजह यह बताई जाती है कि वे लोग डॉ आंबेडकर के गांधी और कांग्रेस विरोध से चिढ़े हुए थे।। उसी समय आंबेडकर की पुस्तक भी आई थी कि व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन फार अनटलेबल्स और पाकिस्तान एंड पार्टीशन आफ इंडिया।
लेकिन आंबेडकर 29 अगस्त 1947 को फिर संविधान सभा में आते हैं। इसके पीछे की अलग कहानी है। आंबेडकर ने संविधान सभा में शामिल होने के लिए लंदन से दिल्ली तक नैतिक और राजनैतिक दबाव भी बनाने की कोशिश की। उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली से भी संपर्क किया। लेकिन उन्होंने कहा कि संविधान निर्माण भारत का अपना मामला है इसलिए आप कांग्रेस के नेताओं से ही संपर्क करें।
दूसरे गोलमेज सम्मेलन में लंदन के किंग्सले हाल में गांधी की मेजबानी करने वाली मुरियल लिस्टर क्वेकर समूह की सदस्य थीं। उस समूह के लोग यह चाहते थे कि भारत में चलने वाला गांधी और आंबेडकर का विवाद समाप्त हो और आजाद भारत के निर्माण में दोनों नेता अपना योगदान दें। इसी सिलसिले में डॉ आंबेडकर के मराठी जीवनीकार सीबी खैरमोड ने लिखा है कि मुरियल लिस्टर 1946 में भारत में थीं। उनका समूह सांप्रदायिक दंगों को शांत कराने में गांधी की मदद कर रहा था। मुरियल और गांधी के बीच कलकत्ता में हुई बातचीत के आधार पर मुरियल ने आंबेडकर से कहा कि गांधी चाहते हैं कि आप नेहरू मंत्रिमंडल के सदस्य बनें और संविधान निर्माण में अपना योगदान दें।
आंबेडकर ने इस संदेश का सकारात्मक जवाब दिया और कहा भी कि वे महज विरोध के लिए विरोध नहीं करना चाहते। वे समझते हैं कि वे अनुसूचित जाति यानी दलित समाज की सेवा सरकार में रहकर ज्यादा कर सकते हैं। उन्हें इस बात की चिंता थी कि सरकार में दलित समाज के लोग नहीं हैं और सवर्ण समाज के लोग हैं जो उन पर अत्याचार करते हैं। इसलिए सरकार में दलित समाज को रहना चाहिए।
भारतीय संविधान और डॉ आंबेडकर की भूमिका के बारे में या तो विवाद खड़ा किया जाता है या फिर व्यापक सरलीकरण किया जाता है। इसके अपने राजनीतिक कारण भी हैं और ईर्ष्या द्वेष भी बड़ी वजह है। एक तरफ डॉ आंबेडकर को संविधान का निर्माता बताया जाता है और बाकी दूसरे लोगों की भूमिका को गौण कर दिया जाताहै तो दूसरी ओर उन्हें संविधान सभा के अन्य सदस्यों जैसा सामान्य सदस्य बताकर उन पर हमले किए जाते हैं।
आइए इस मिथक और विवाद की सच्चाई को विभिन्न कोणों से जांचते हैं। पहली बात तो यह है कि संविधान बनाने का सारा श्रेय डॉ आंबेडकर लेने को तैयार ही नहीं हैं। वे इतने आब्जेक्टिव और विनम्र हैं कि फर्जी दावे में उनकी यकीन नहीं है। बल्कि उन्हें संविधान बनाने के लिए कड़ी मेहनत करने का श्रेय देने वाले दूसरे लोग हैं। ऐसे लोगों में पंडित जवाहर लाल नेहरू स्वयं शामिल हैं।
लेकिन पहले यह देख लेते हैं कि दो साल 11 महीने और 18 दिन की बैठक के बाद जब 25 नवंबर 1949 को संविधान का आखिरी मसविदा पारित हुआ तो उस मौके पर दिए गए भाषण में आंबेडकर ने क्या कहा।
उन्होंने कहा, “संविधान बनाने का जो श्रेय मुझे दिया जाता है वह मुझे नहीं दिया जाना चाहिए। इसका एक हद तक श्रेय जाता है बी.एन राव को। जिन्होंने कच्चा मसविदा बनाकर दिया। वे संविधान सभा के सलाहकार थे। फिर श्रेय जाना चाहिए मसविदा समिति के उन लोगों को जिन्होंने 141 दिन तक बैठकें कीं। इसके अलावा संविधान के मुख्य मसविदा लेखक थे सुरेंद्र नाथ मुखर्जी। उन्होंने समविदा समिति में काम करते हुए बहुत सरल भाषा में अनुच्छेदों को लिखा।’’
संविधान की रचना में डॉ आबेडकर का क्या योगदान था इस बारे में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की टिप्पणी भी ध्यान देने लायक है। छह दिसंबर 1956 को जब डॉ आंबेडकर का निधन हुआ तो नेहरू ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा, “अक्सर कहा जाता है कि वे हमारे संविधान निर्माताओं में से एक हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि संविधान निर्माताओं में उनसे ज्यादा मेहनत किसी ने नहीं की और न ही किसी ने उतने कष्ट उठाए।’’(writings and speeches of Ambedkar Vol. 15. Page. 976)
मसविदा समिति के तमाम सदस्य बहुत सी बैठकों में अनुपस्थित रहते थे। ऐसे में डॉ आंबेडकर पर काम का काफी बोझ उठाना पड़ जाता था।उनका काम लंबा मसविदा तैयार करके ही नहीं समाप्त हुआ। उन्हें संविधान सभा की बहसों का जवाब देना होता था। उन्हें यह फैसला करना होता था कि संशोधनों को स्वीकार कर लिया जाए या न स्वीकार किया जाए। संविधान सभा एक प्रकार से संसद ही थी। इसलिए इतने बड़े काम को करना एक बेहतरीन प्रदर्शन था।(Narendra chapalgaonkar, Mahatma Gandhi and Indian Constituion, pp. 25)
संविधान निर्माण के माध्यम से भारत में सामाजिक क्रांति व प्रशानिक ढांचा तैयार करने में डॉ आंबेडकर की भूमिका के महत्त्व को रेखांकित करते हुए प्रोफेसर एम.एल कसारे ने लिखा है कि उन्होंने संविधान सभा की कम से कम दस कमेटियों में अपना योगदान दिया। संविधान सभा के सदस्य होने के साथ वे जिन समितियों के सदस्य थे उनके नाम इस प्रकार हैः—
- मसविदा समिति के अध्यक्ष
- सलाहकार समिति के सदस्य
- अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष
- मौलिक अधिकारों की उपसमिति के सदस्य
- केंद्रीय संविधान समिति के सदस्य
- नागरिकता संबंधी अस्थायी समिति के सदस्य
- राष्ट्रीय ध्वज की अस्थायी समिति के सदस्य
- सुप्रीम कोर्ट संबंधी अस्थायी समिति के सदस्य
डॉ आंबेडकर चूंकि बी.एन. राव और दूसरे लोगों की तरह से सिर्फ संविधानविद ही नहीं एक समाज सुधारक और दलित समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले एक क्रांतिकारी चिंतक भी थे इसलिए भले ही उन्होंने संविधान का दर्शन और उसका ढांचा यूरोपीय प्रेरणा से अनुप्राणित रहा हो लेकिन उन्होंने उसे भारत की समस्याओं के लिहाज से व्यावहारिकता प्रदान करने की कोशिश भी की। वे एक ओर संविधान के माध्यम से समाज में जाति और वर्ग में व्याप्त ऊंच नीच का भेद मिटाना चाहते थे तो दूसरी ओर भारत को एक ऐसे मजबूत राष्ट्र के रूप में स्थापित करना चाहते थे जिसकी आजादी फिर कोई नहीं छीन सके। उनकी यह चिंता उनके 25 नवंबर के भाषण में परिलक्षित होती है।
वे उस भाषण में बार बार यह सवाल उठाते हैं कि भारत का भविष्य क्या होगा? उसकी आजादी का क्या होगा?क्या भारत की आजादी कायम रहेगी या वह इसे फिर से गंवा देगा। क्योंकि भारत हमेशा आजाद नहीं रहा है। एक बार उसकी आजादी गई है तो क्या दोबारा भी जाएगी।
इसके बाद वे सवाल करते हैं कि क्या भारत के लोग मजहब को देश से ऊपर रखेंगे? उनकी साफ चेतावनी है कि अगर पार्टियों ने धर्म या मजहब को देश से ऊपर रखा तो हमारी आजादी संकट में पड़ जाएगी और फिर हमेशा के लिए खो जाएगी।
फिर वे सवाल करते हैं कि क्या भारत अपने लोकतंत्र को कायम रख पाएगा? ऐसा नहीं है कि भारत में पहले लोकतंत्र नहीं रहा है। वहां गणराज्य थे। अगर राजतंत्र था तो यहां राजा चुने जाते थे। वे कहते हैं कि भारत में संसदीय प्रक्रिया का विकास हुआ। बौद्ध भिक्षु संघ के अध्ययन से यही निकलता है। आधुनिक युग की सभी संसदीय प्रक्रियाएं संघ में पालन की जाती थीं। Motions, Resolutions, Quorum, Whip, Counting of votes, voting by ballot, Census Motion, Regularization, Res Judicata की व्यवस्थाएं पहले से थीं। वे कहते हैं कि बुद्ध अपनी सभाओं में इन नियमों का पालन करते थे। इन नियमों को उन्होंने देश में चलने वाली व्यवस्थाओं से प्राप्त किया था।
फिर वे सवाल करते हैं कि क्या भारत दोबारा अपना लोकतंत्र खो देगा? वे इसके जवाब में कहते हैं कि अगर हमें लोकतंत्र का ढांचा ही नहीं उसका सार भी चाहिए तो हमें सत्याग्रह, असहयोग और सिविल नाफरमानी बंद करनी होगी। जब तक संवैधानिक रास्ते मौजूद हैं तब तक इनकी जरूरत नहीं है। फिर वे जान स्टूअर्ट मिल का उल्लेख करते हुए कहते हैं—जिन्हें भी लोकतंत्र कायम रखना है उन्हें अपनी आजादी किसी भी महापुरुष के चरणों में समर्पित नहीं करनी चाहिए। न ही उसे इतनी ताकत देनी चाहिए जिससे संस्थाएं नष्ट हो जाएं। फिर वे जोर देते हुए कहते हैं कि इस लोकतंत्र को टिकाए रखने के लिए सामाजिक लोकतंत्र अति आवश्यक है।
आंबेडकर संविधान के तीन महान मूल्यों की लोकतंत्र के लिए अनिवार्यता को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि समता स्वतंत्रता और बंधुत्व को अलग अलग नहीं समझना चाहिए।अगर हम इन्हें अलग करेंगे तो लोकतंत्र हार जाएगा।क्योंकि समता के बिना स्वतंत्रता कुछ लोगों को ज्यादा लोगों पर हावी कर देगी।स्वतंत्रता के बिना समता व्यक्तिगत पहल या उद्म को समाप्त कर देगी।बंधुत्व के बिना दोनों स्वाभाविक नहीं रहेंगी।
यहां आंबेडकर की उस प्रसिद्ध चेतावनी का उल्लेख भी करना आवश्यक है जो सामाजिक क्रांति के दर्शन से अनुप्राणित है। वे कहते हैं, “ 26 जनवरी 1950 को हम अंतर्विरोधों के जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। एक ओर राजनीतिक बराबरी है तो दूसरी ओर सामाजिक जीवन में गैर बराबरी है। अगर राजनीतिक जीवन में हमें एक व्यक्ति और एक वोट का मूल्य हासिल है तो सामाजिक आर्थिक जीवन में हम एक व्यक्ति और एक मूल्य के सिद्धांत से इनकार कर रहे हैं।’’
हमारे संविधान की उद्देशिका में राष्ट्रीय जीवन के लिए बेहद प्रमुख मूल्यों और सिद्धांतों का उल्लेख है। आमतौर पर यह माना जाता है कि उसकी रचना भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने की थी। लेकिन हाल में आकाश सिंह राठौर नाम के एक स्कॉलर ने आंबेडकरस प्रिएंबल नाम की एक पुस्तक के माध्यम से यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि 1976 से पहले उसका जो भी स्वरूप था उसे अंतिम रूप डॉ आंबेडकर ने दिया था। आकाश सिंह राठौर का कहना है हालांकि इसके कोई लिखित साक्ष्य नहीं हैं लेकिन अगर आप आंबेडकर के विचारों और उसमें चुने जाने वाले शब्दों का अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि वह उन्हीं के दिमाग की उपज है।
वे सिद्धात हैः–
न्याय(Justice)
स्वतंत्रता(Liberty)
समता(Equality)
बंधुत्व(Fraternity)
गरिमा(Dignity)
राष्ट्र(Nation)
आकाश सिंह राठौर का मानना है कि आंबेडकर ने संविधान सभा को 20,000 शब्दों का एक ज्ञापन दिया था।उसमें अल्पसंख्यकों के अधिकारों और उन्हें कैसे हासिल किया जाए उसका वर्णन था।जब यह संविधान सभा में स्वीकार नहीं हुआ तो उन्होंने इसे पुस्तक के रूप में छपवा दिया।यह एक किस्म का सैद्धांतिक समाजवादी दस्तावेज है।बाद में उन्होंने इसे प्रस्तावना में जुड़वा दिया।राज्य के नीति निदेशक तत्व में भी जो समाजवादी तत्व हैं उन पर भी आंबेडकर के स्टेट एंड माइनरिटीज का प्रभाव बताया जाता है।अगर बी एन राव के प्रारूप में दी गई उद्देशिका को देखेंगे और पंडित नेहरू द्वारा दिए गए प्रस्ताव को देखेंगे और बाद मे जो संविधान में लिया गया उसे देखेंगे तो पाएंगे कि उद्देशिका को तराशने का काम आंबेडकर ने बखूबी किया है।
वास्तव में संविधान निर्माण से डॉ आंबेडकर के खींचतान के संबंध हैं। सन 1953 में वे राज्यसभा में कहते हैं, “धारणा यही है कि डॉ आंबेडकर संविधान के मुख्य रचयिता हैं। उसके विपरीत मैं एक वेतनभोगी कर्मचारी था। मैंने वही किया जो मुझसे करने को कहा गया। यह सब मेरी इच्छा के विरुद्ध था।’’
उसके बाद आंबेडकर एक जगह यह भी कहते हैं कि मैंने इसे बनाया था लेकिन यह हमारी आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतर रहा है इसलिए इसे मैं ही जलाऊंगा।
लेकिन 1955 में वे कहते हैं कि देश को जो संविधान दिया गया है वह अनोखा दस्तावेज है।
संविधान पर गांधी की सलाहः—
वैसे तो 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन ने जो प्रस्ताव पारित किया था उसमें नागरिक अधिकारों का उल्लेख था। उन्हीं नागरिक अधिकारों को संविधान में मौलिक अधिकारों के रूप में शामिल किया गया। उसके पीछे महात्मा गांधी का चिंतन साफ था। इसलिए नागरिकों के लिहाज से संविधान के सबसे महत्त्वपूर्ण हिस्से में तो महात्मा गांधी मौजूद हैं।लेकिन केंद्रीकृत संविधान बनाने के विरुद्ध महात्मा गांधी का जो सुझाव था उसे संविधान सभा ने स्वीकार नहीं किया। यह भी बात साफ है। गांधी चाहते थे कि विधासभा और संसद के लिए प्रत्यक्ष चुनाव न हो बल्कि सिर्फ ग्राम पंचायतों का चुनाव प्रत्यक्ष हो। गांधी नहीं चाहते थे कि राज्य की समस्त शक्तियां संसद और विधानसभाओं में केंद्रित हों। वे एक विकेंद्रित व्यवस्था के लिए संविधान चाहते थे। संविधान सभा ने उस पर चर्चा की लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया। संविधान सभा में गांधी के कई अनुयायी थे। उन्होंने उस बात को उठाया। स्वयं संविधान सभा के अध्यक्ष बाबू राजेंद्र प्रसाद ने उस मसले को उठाया पर उनकी भी नहीं सुनी गई। कहते हैं कि ग्राम पंचायतों को महत्त्व न देने के मामले पर नेहरू और आंबेडकर एक थे। आंबेडकर मानते थे कि गांव अन्याय, गंदगी और अज्ञानता के केंद्र हैं।
रोचक तथ्य यह है कि वर्धा में श्रीमन नारायण अग्रवाल नाम के एक प्राचार्य महोदय स्वतंत्र भारत के लिए एक गांधीवादी संविधान तैयार भी कर डाला था। उन्होंने उसे गांधी को दिखाया और उस पर गांधी से भूमिका लिखवाई। उस पुस्तक का नाम था गांधियन कांस्टीट्यूशन फार फ्री इंडिया।
श्रीमन नारायण अग्रवाल के संविधान पर गांधी ने लिखाः—
इसे गांधीवादी संविधान कहना ठीक नहीं है। यह ठीक है कि अग्रवाल का फ्रेम मेरे लेखन पर आधारित है। इसे मेरे देखने के लाभ हैं पर नुकसान भी है। इससे लगेगा कि सब कुछ मेरा ही विचार है। मैं ऐसी गलती के लिए चेतावनी देता हूं। अगर मैं हर शब्द से सहमत होता तो इसे मैं खुद लिखता। मैंने इसे दो बार पढ़ा है पर इसके हर शब्द को मैं जांच नहीं सका हूं। हालांकि लेखक ने वे संशोधन कर दिए हैं जो मैं चाहता था। लेखक ने कोई व्यापक संविधान नहीं बनाया है। उन्होंने एक रूप रेखा प्रस्तुत की है। रोचक बात यह है कि गांधी ने यह भूमिका 30 नवंबर 1945 को कलकत्ता जाते समय ट्रेन में लिखी थी।
श्रीमन नारायण अग्रवाल ने इसके आमुख में लिखा है कि भारत संवैधानिक विकास की प्राचीन प्रयोगशाला है। यहां स्वराज्य, वैराज्य, राष्ट्रिका, द्वैराज्य, अराजक जैसे सिद्धांतों की उपस्थिति बहुत पहले से है। अगर हम काशी प्रसाद जयसवाल की हिंदू राजनीतिक व्यवस्था को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि यहां की राज्य व्यवस्था विकसित थी। इसलिए हमें पश्चिमी संविधान की नकल करने के बजाय देशी संविधान बनाना चाहिए। उनकी चेतावनी थी कि बाहर का ढांचा लाए तो यह भारत का अपमान होगा क्योंकि संविधान निर्यात की वस्तु नहीं है।
संविधान का जो मसविदा 26 फरवरी 1948 को सामने आया उसमें गांधी के विकेंद्रीकरण की बात कौन करे पंचायत शब्द ही नहीं आया। इस पर राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने आपत्ति की। अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने कानूनी सलाहकार बीएन राऊ को लिखा कि मुझे अच्छा लगेगा अगर यह मसविदा गांव से शुरू होकर केंद्र तक जाए। क्योंकि गांव बहुत पहले से इस देश की इकाई रहा है और आगे भी रहने वाला है।राजेंद्र बाबू ने कहा कि प्रांतीय और केंद्रीय सरकारों का ढांचा वैसा ही रखते हुए आवश्यक अनुच्छेद गढ़े जाने चाहिए। उन्होंने कहा, “मैं इस बात की जोरदार वकालत करता हूं कि वयस्क मताधिकार का प्रयोग सिर्फ ग्राम पंचायत के लिए किया जाए और गांव पंचायतों के इलेक्टोरल कॉलेज का इस्तेमाल प्रांत और केंद्र की सरकारों को चुनने के लिए किया जाए। प्रसाद ने यह भी दिलाया कि महीने भर पहले ही कांग्रेस कमेटी ने ऐसा संविधान स्वीकार किया है जिसमें पंचायत को आधार बनाया गया है। लेकिन राऊ ने राजेंद्र प्रसाद के सुझाव को सख्ती से खारिज कर दिया।
नवंबर में जब संविधान सभा ने मसविदा प्रस्ताव पर बहस शुरू की जो गांधी के पंचायतों का विचार आया इसमें सिब्बन लाल सक्सेना और एम.ए अय्यंगर प्रमुख हैं। आखिरकार गांधी के पंचायत का विचार राज्य के नीति निदेशक तत्व के अनुच्छेद 40 में स्थान पा सका। संविधान सभा ने गांधी को उस समय जोरदार तरीके से याद किया जब अस्पृश्यता निवारण अनुच्छेद 17 पारित किया गया।
वास्तव में गांधी और आंबेडकर की तुलना अगर संवैधानिक ढांचे के निर्माण और राज्य की संस्थाओं के आधार पर करेंगे तो दोनों में बहुत अंतर पाएंगे। हमें यह भी लग सकता है कि गांधी हार गए और आंबेडकर जीत गए।
आंबेडकर कानून और संवैधानिक ढांचे पर बहुत ज्यादा यकीन करते थे। जबकि महात्मा गांधी हृदय परिवर्तन और प्रायश्चित पर विश्वास करते थे। आंबेडकर कानून बनाकर जाति व्यवस्था मिटाना चाहते थे। वे हिंदुओं के लिए एक धर्म ग्रंथ चाहते थे।
जबकि गांधी नैतिक और आध्यात्मिक बोध के आधार पर अन्याय को मिटाना चाहते थे। गांधी पाप और पुण्य की भाषा बोलते थे और आंबेडकर कानूनी और गैर कानूनी। आंबेडकर ने एक जगह कहा भी है कि विधायिका का यह कर्तव्य है कि वह आप को भोजन वस्त्र, आवास, शिक्षा, दवाई और आजीविका के सारे साधन प्रदान करे। कानून बनाने का काम आप की सहमति, मदद और इच्छा से होना चाहिए। संक्षेप में आप के समस्त सांसारिक सुखों का रहवासधाम कानून में ही है। आप को सत्ता और कानून निर्माण की प्रक्रिया पर कब्जा करना होगा। इसलिए यह आप का कर्तव्य है कि आप अपना ध्यान उपवास पूजा और प्रायश्चित से हटा कर कानून निर्माण की शक्ति पर कब्जा करने लगाएं।इसी मार्ग में आपकी मुक्ति है।
लेकिन अंत में इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि जिस सामाजिक नैतिकता की बात गांधी करते थे उसी की तलाश में डा आंबेडकर ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। उनका कहना था कि धर्म के माध्यम से ही समाज में वह नैतिकता पैदा की जा सकती है जो कि कानून के राज और संविधान को धारण कर सके। वे कोलंबिया विश्वविद्यालय के अपने गुरु और प्रैगमटिक फिलास्फर प्रोफेसर जान डेवी के हवाले से कहते हैं कि लोकतंत्र के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है और उससे भी ज्यादा जरूरी है संवैधानिक नैतिकता। वे मानते थे कि लोकतंत्र महज सरकार का चुना जाना नहीं है। वह एक सम्मिलित जीवन है। मनुष्य अपने सामाजिक वातावरण का उत्पाद भी है और एजेंट भी जो उसे संवाद और शिक्षा से प्राप्त होता है।
गांधी का भी सारा जोर बंधुत्व और प्रेम पर ही है। कोई भी संविधान हिंसक और अनैतिक वातावरण में सफल नहीं हो सकता। इस मायने में गांधी और आंबेडकर में एक गहरा सामंजस्य ढूंढा जा सकता है।
प्रोफेसर अरुण कुमार त्रिपाठी जी का यह व्याख्यान “महात्मा गांधी और डॉ. अंबेडकर: सामंजस्य की संभावनाएँ” विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार में प्रस्तुत किया गया। यह सेमिनार आईटीएम यूनिवर्सिटी, ग्वालियर में 29 नवंबर से 1 दिसंबर 2024 तक आयोजित हुआ।
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.