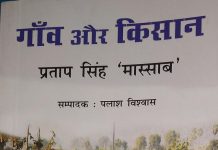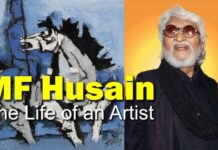— परिचय दास —
वह न मौन था, न वाणी। वह न कोई विचार था, न उसका प्रतिवाद। वह केवल एक चलती हुई करुणा थी—जल की तरह, वायु की तरह, ज्योति की तरह। उसे बुद्ध कहते हैं। पर वह कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं—वह तो उस क्षण का अनुभव है जब भीतर सब रुक जाता है और बाहर सब स्पष्ट हो जाता है।
वह एक दिन महलों से निकला था पर उस पल जो उसने देखा, वह केवल एक वृद्ध, एक रोगी और एक मृत देह नहीं थी—वह मनुष्य की सीमाओं की नंगी तस्वीर थी और वहाँ से उसने लौटना नहीं चुना। यह लौटना नहीं था, यह उतरना था—दुनिया की सतह से नीचे, अपने भीतर की खोहों में, जहाँ इच्छाएँ साँपों की तरह लिपटी थीं, जहाँ अहंकार अंधेरे की तरह फैला था।
बुद्ध ने धर्म को किसी आकाशीय सत्ता से जोड़ा ही नहीं। उन्होंने देवताओं को नकारा नहीं पर उन्हें अंतिम नहीं माना। उन्होंने कहा, “अप्प दीपो भव”। कोई दया नहीं देगा, कोई मुक्त नहीं करेगा। यह जो जीवन है—तुम्हारी साँस, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारा मौन—इसी में मुक्ति का द्वार है।
ध्यान उनका हथियार नहीं था, कोई यौगिक चमत्कार नहीं। वह तो आत्मा के ऊपर जमी धूल को हटाने की नमी थी। वह एक ऐसा मौन था जो चीखता नहीं पर सुनाई पड़ता है। उनका ध्यान कोई अनुशासन नहीं, कोई अभ्यास नहीं—वह एक सहजता थी। जैसे फूल खिलता है, जैसे ओस गिरती है, वैसे ही ध्यान आता है—यदि तुम प्रतीक्षा कर सको, यदि तुम उपस्थित हो सको।
वे किसी युद्ध में नहीं थे पर उनके मौन ने युद्धों को परास्त किया। वे किसी ताज के दावेदार नहीं थे पर उनके चरणों में सम्राट झुके। वे धर्म का प्रचार करने नहीं चले पर उनकी करुणा इतनी प्रबल थी कि वह लहर की तरह बढ़ती चली गई। उनके शब्द, उनके संकेत, उनकी दृष्टि—सब कुछ इतना पारदर्शी था कि हर युग ने उसमें अपने प्रश्न के उत्तर खोज लिए।
उनकी करुणा भावुक नहीं थी, उनकी दृष्टि दार्शनिक नहीं थी। वे न तो किसी संप्रदाय की घोषणा थे, न किसी मत की प्रणाली। वे तो बस एक सादगी थे—इतनी गहरी कि उसमें हर जटिलता घुल जाए।
बुद्ध जानते थे कि दुःख है और यह जानना कोई शिकायत नहीं थी—यह तो मनुष्य होने की पहली स्वीकृति थी। उन्होंने दुःख को दोष नहीं कहा, उन्होंने उसे देखा, समझा, और पूछा कि इसे मिटाया कैसे जाए। उनका यह प्रश्न ही उनकी क्रांति था।
न उन्होंने किसी स्वर्ग की लालसा की, न किसी नरक का भय दिया। वे समय से परे गए पर यहीं रहे—गांवों में, रास्तों पर, पीपल के नीचे, गरीबों के द्वार पर। उन्होंने धर्म को सरल किया, जैसे कोई जटिल संगीतमय राग एक माँ की लोरी बन जाए।
बुद्ध का चेहरा एक वक़्त नहीं है, वह हर युग का चेहरा है। वह तसल्ली नहीं देता, वह प्रश्न खड़े करता है। वह उत्तर नहीं देता, वह देखने की दृष्टि देता है और यही उनका होना है—एक ऐसा मौन जो अब भी गूंजता है, एक ऐसी दृष्टि, जो अब भी राह दिखाती है।
वे गए नहीं, वे ठहर गए हैं—हर उस आँख में जो भीतर झांकती है, हर उस हृदय में जो जगत से नहीं, स्वयं से संवाद करता है। बुद्ध आज भी वही हैं—न संप्रदाय, न मूर्ति, न मन्त्र—केवल एक सरल, सुंदर, और सम्यक मनुष्य।
बुद्ध की उपस्थिति किसी समयबद्ध आख्यान में नहीं बँधती। वे बीते हुए नहीं हैं, वे किसी ग्रंथ की पीली होती पृष्ठभूमि नहीं—बल्कि वे वर्तमान की सबसे सजीव चेतना हैं। जब कोई मनुष्य पहली बार स्वयं को देखता है, बिना मूल्यांकन के, बिना अपराधबोध के—वहाँ बुद्ध होते हैं।
बुद्ध की राह में न कोई चमत्कार था, न कोई दिव्य उद् घोष। वह तो एक सहज चलना था—जैसे कोई नदी पहाड़ों को छोड़ मैदानों की ओर बढ़ती है। उनका जीवन एक प्रयोगशाला था और वे स्वयं उस प्रयोग के विषय भी थे, प्रयोगकर्ता भी। उन्होंने अपने अनुभव को किसी पर थोपा नहीं, बल्कि उसे इस तरह प्रस्तुत किया कि सुननेवाला उसे अपना अनुभव बना सके।
जब वे बोले—तो उनकी वाणी में वज्र की निश्चयता थी और फूल की कोमलता। वे कहते हैं—”संपज्जानो सतिमा”—जागरूक रहो, सजग रहो। यह सजगता किसी बाहरी अनुशासन से नहीं आती, यह भीतर की एक चिंगारी से जन्मती है जो देखती है पर पकड़ती नहीं; जो जानती है, पर दावा नहीं करती।
बुद्ध की करुणा एक महान कल्पना नहीं थी—वह उनकी जीवित चेतना थी। यह करुणा आँखों में नहीं, हाथों में थी—वहाँ, जहाँ उन्होंने अंगुलिमाल को रोका, किसी पतिता को छूकर उसकी गरिमा लौटाई, किसी डरे हुए ब्राह्मण को प्रेम से देखा। यह करुणा आदेश नहीं देती, यह अवसर देती है।
बुद्ध का धर्म तर्क और आत्मा के मध्य का एक सेतु है। वे कहते हैं, कोई बात केवल इसलिए मत मानो कि वह परंपरा में है या किसी ज्ञानी ने कही है। उसे जाँचो, देखो और फिर यदि वह तुम्हें भीतर से हल्का करे, शांत करे तो स्वीकारो।
उनकी दृष्टि में कोई भेद नहीं था—न जाति का, न वर्ण का , न लिंग का, न संप्रदाय का। वे एक ऐसे स्वप्न की शुरुआत थे, जहाँ मनुष्य को मनुष्य की तरह देखा गया—बिना लेबल, बिना डर, बिना अपेक्षा। यह उस युग में कितना बड़ा विचार था, यह समझना आज के लिए भी उतना ही कठिन है।
उन्होंने मृत्यु को अस्वीकार नहीं किया—पर उन्होंने उसे दुःख का कारण भी नहीं माना। उनके लिए मृत्यु जीवन की ही एक लहर थी जो लौटकर नहीं आती पर हर बार नया रंग लेकर आती है। जीवन के प्रति यह निर्मम और कोमल दृष्टि एक साथ होना ही बुद्धत्व है।
बुद्ध ने जो कहा, वह कम है। जो नहीं कहा—वह अधिक। वह मौन जो उन्होंने प्रश्नों के उत्तर में दिया—वह गूंजता है। वही मौन आज के कोलाहल में एक पुकार बनकर लौटता है—कि थमो, देखो, होश में आओ।
बुद्ध, वस्तुतः, किसी देवता की प्रतिमा नहीं हैं। वे भीतर के अंधकार में दीप्त एक ज्योति हैं जो कहती है—तुम भी बुद्ध हो सकते हो। यह ‘हो सकना’ ही सबसे बड़ी क्रांति है। यह तुम्हारे भीतर की संभावना का उद् घाटन है, जिसे न कोई गुरु देता है, न कोई ग्रंथ, केवल तुम्हारा देखना।
बुद्ध, शब्द नहीं—दृष्टि हैं। वे उत्तर नहीं—पथ हैं। वे धर्म नहीं—ध्यान हैं और इसलिए वे हर युग में लौटते हैं, हर प्रश्न में जन्म लेते हैं और हर मौन में समाधि बन जाते हैं।
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.