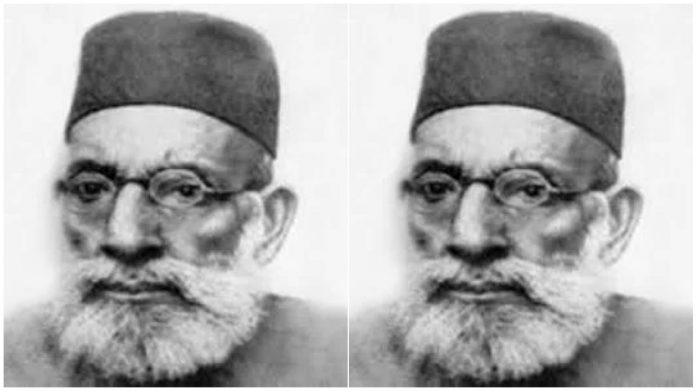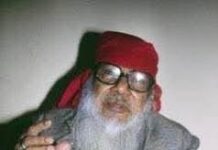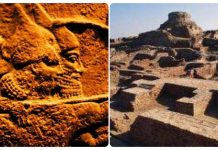— परमजीत जज —
मौजूदा उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मोहान गांव में 1875 में जनमे कवि-राजनेता मौलाना हसरत मोहनी अपने राजनीतिक नजरिये में उस हद तक उदार रहे, जिस हद तक सोचा जा सकता है। उनकी शायरी ने तो उन्हें अमर कर दिया, लेकिन इतिहास ने उन्हें एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में भुला ही दिया है। उन्होंने ही “इंक़लाब ज़िंदाबाद” का नारा गढ़ा था। उस समय अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से मशहूर एमएओ कॉलेज में अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद वह कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गये और कांग्रेस में गरम दल कहे जाने वाले गुट का पक्ष लिया था, जिसकी अगुवाई बाल गंगाधर तिलक कर रहे थे। हालांकि मोहानी लंबे समय तक कांग्रेस के साथ नहीं रहे और कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गये। उन्होंने 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी के पहले पार्टी कार्यालय का उदघाटन किया था और वहां “लाल झंडा लहराया था।”
मोहानी उसी साल दिसंबर में कानपुर में आयोजित कम्युनिस्टों के पहले अखिल भारतीय सम्मेलन की स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। कम्युनिस्ट पार्टी से निकाले जाने के बाद उन्होंने अपनी “आज़ाद पार्टी” का गठन किया। वह मुस्लिम लीग का भी हिस्सा बने, लेकिन 1936 में दो-राष्ट्रों के सिद्धांत को खारिज करने के बाद इसे उन्होने छोड़ दिया। 1947 में नया-नया देश बने पाकिस्तान जाने की उनकी इच्छा कभी नहीं रही।
मोहानी को उनके राजनीतिक जुड़ाव के लिहाज़ से विरोधाभासी कार्यों के संयोजन के रूप में समझा जा सकता है। फिर भी, वह ख़ासतौर पर उन मूल्यों को लेकर प्रतिबद्ध रहे, जिन्हें उन्होंने एक स्वतंत्र भारतीय समाज और सरकार को लेकर इंसाफ़ पसंद होने के रूप में परिभाषित किया था। इनमें सांप्रदायिक सौहार्द, श्रमिकों और किसानों के हितों की रक्षा और लोकतांत्रिक मूल्य शामिल हैं।
हम मोहानी के दिखायी देने वाले इन विरोधाभासी कार्यों और बदलते वैचारिक संदर्भों को एक कवि और राजनीतिक कार्यकर्ता की प्रतिक्रिया के रूप में विशिष्ट परिस्थितियों में सामाजिक ताकतों में संरचनात्मक परिवर्तनों के रूप में समझ सकते हैं, यानी कि इन परिवर्तनों को लेकर उनके दोहरे विचार वाले भाव उनकी एक अंतर्निहित विशेषता है। उनका कहना था कि तीन “M” उनके दिल के बेहद क़रीब था। इन तीन एम में पहला एम मक्का था, और उन्होंने कई बार हज यात्रा की थी; दूसरा एम था मथुरा, जहां वह हर साल कृष्ण अष्टमी के मौक़े पर जाया करते थे; और तीसरा एम वह मास्को था, जो भारत में सोवियत शैली के ग्रामीण गणराज्यों के पक्ष में संविधान सभा में उनके तर्कों का आधार था।
संविधान सभा में हुई बहस और अल्पसंख्यक
मोहानी संविधान सभा के लिए चुने गये थे और उन्होंने संविधान सभा में होने वाली बहसों में भाग लिया था, लेकिन संविधान के प्रारूप को लेकर असंतुष्ट होने की वजह से उन्होंने प्रारूप संविधान पर कभी हस्ताक्षर नहीं किये। 13 मई,1951 को लखनऊ में उनका निधन हो गया, और उनकी क़ब्र आज भी कई आगंतुकों के लिए आकर्षण की एक जगह बनी हुई है। उनके बेटे मौलाना नुसरत मोहानी ने पाकिस्तान के कराची में हसरत मोहानी मेमोरियल सोसाइटी की स्थापना की है, जो उनकी पुण्यतिथि पर आज भी उन्हें याद करते हुए बैठकें करती रहती है।
मोहानी संविधान सभा की बहसों के शुरुआती दौर में काफ़ी मुखर थे, और संविधान सभा के दूसरे सदस्य उनकी टिप्पणियों का मज़ाक उड़ाया करते थे। एक मौक़े पर तो संविधान सभा के अध्यक्ष को सभा के उन सदस्यों को याद दिलाना पड़ा था कि मोहानी उनमें वरिष्ठ सदस्य हैं और एक पुराने स्वतंत्रता सेनानी हैं। हालांकि, मोहानी ने कभी भी उन नकारात्मक टिप्पणियों पर किसी तरह का कोई जवाब देने की ज़हमत नहीं उठायी थी। विधानसभा में उनके कई हस्तक्षेपों में से एक हस्तक्षेप अल्पसंख्यकों से जुड़े सवालों को लेकर था, और ये सवाल आज भी बेहद प्रासंगिक हैं।
4 जनवरी 1949 को जब संविधानसभा अनुच्छेद 67 पर बहस कर रही थी, तो उन्होंने इस अनुच्छेद को अनुच्छेद 293 से जोड़े जाने पर आपत्ति जतायी थी, जिसमें अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था। एक दिलचस्प हस्तक्षेप में उन्होंने कहा था, “मैं सीटों के आरक्षण का कड़ा विरोध करता हूं और किसी भी परिस्थिति में आरक्षण नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूं कि जब हमने संयुक्त निर्वाचक मंडल और वयस्क मताधिकार का प्रावधान कर लिया है, ऐसे में तो आरक्षण की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। दोनों एकसाथ नहीं हो सकते। जब मतदाता संयुक्त होंगे, तो इसका मतलब तो यही होगा न कि हर एक व्यक्ति को हर एक निर्वाचन क्षेत्र से खड़े होने और चुनाव लड़ने का अधिकार होगा। सांप्रदायिक आधार पर आप इसके दायरे को सीमित कर रहे हैं, क्योंकि आप पहले ही कह चुके हैं कि आप मुसलमानों को आरक्षण इसलिए देना चाहेंगे, क्योंकि वे अल्पसंख्यक हैं। मैं अनुसूचित जातियों के बारे में नहीं जानता, लेकिन मेरे एक मित्र ने अभी-अभी कहा है कि आप उन्हें कोई आरक्षण नहीं देना चाहेंगे। फिर आप मुसलमानों को अल्पसंख्यक क्यों कहते हैं? उन्हें अल्पसंख्यक तभी कहा जा सकता है, जब वे एक सांप्रदायिक निकाय के रूप में कार्य करें। जब तक मुसलमान मुस्लिम लीग में थे, तभी तक वे अल्पसंख्यक थे।”
जब संविधान सभा ने धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण के प्रावधान को ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया, तो संविधान सभा के इस क़दम ने मोहानी के उसी नज़रिये की पुष्टि की थी। हालांकि, मोहानी की दलील का अहम पहलू मुसलमानों के अल्पसंख्यक होने को लेकर था। जब तक कि मुसलमान लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं, तब तक उन्होंने मुसलमानों को अल्पसंख्यक के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। उनकी दलील थी कि जब तक मुसलमानों की अपनी पार्टी बनी रहेगी, वे अल्पसंख्यक भी बने रहेंगे।
दूसरे शब्दों में मोहानी ने महसूस किया था कि राजनीतिक गुंज़ाइश किसी धार्मिक समुदाय के लोगों के लिए कुछ विकल्प देती है : वे या तो मौजूदा पार्टियों में शामिल होकर राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा बन सकते हैं या फिर बिना किसी सांप्रदायिक मांग या दबाव के एक पार्टी बना सकते हैं। कहा जा सकता है कि मोहानी नागरिकों की नागरिकता को लेकर प्रतिबद्ध थे, हालांकि वह पहले उस मुस्लिम लीग के सदस्य रह चुके थे,जिसके बारे में उनकी स्पष्ट राय थी कि लीग एक ऐसा संगठन था, जिसकी उन्हें कोई आवश्यकता नहीं थी।
25 मई 1949 को सरदार पटेल ने अपनी पिछली रिपोर्ट को जारी करते हुए अल्पसंख्यकों आदि पर सलाहकार समिति की रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए राजनीतिक आरक्षण ख़त्म कर दिया गया था। इस रिपोर्ट पर पटेल ने कहा था कि इसमें सिख समुदाय को एक अपवाद के रूप में रखा गया है। अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण के अनुरूप सिखों की कुछ जातियों को आरक्षण के प्रावधान के तहत शामिल किया जाएगा। इसके बाद हुई बहस में मोहानी ने 26 मई को एक तरह से भविष्यवाणी करते हुए गहरे बयान दिये थे।
उन्होंने कहा था, ‘हम सब मिलकर एक बार और हमेशा के लिए यह तय कर लें कि हमारे बीच कोई सांप्रदायिक दल नहीं होगा। अगर हमें एक सच्चे लोकतांत्रिक देश की स्थापना करनी है, तो इसमें किसी भी धार्मिक या सांप्रदायिक दल के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। जैसा कि सभी जानते हैं, लोकतंत्र का मतलब बहुमत का शासन होता है, और इसलिए, इसका मतलब यह हुआ कि अल्पसंख्यकों को बहुमत के फ़ैसलों के प्रति समर्पण करना होगा। महोदय, अब सवाल उठता है कि अल्पसंख्यकों की ओर से बहुमत के फ़ैसलों के प्रति समर्पण करने की वजह क्या है? वे ऐसा यह मानकर करेंगे कि उनके लिए यह संभव हो सकेगा कि आने वाले दिनों में जनता की राय उनके पक्ष में बदलने के साथ ही वे सरकार की सीट पर कब्ज़ा कर सकें और उस स्थिति में पहले वाला बहुमत अल्पसंख्यक हो जाएगा और पहले वाला अल्पसंख्यक बहुमत बन जाएगा।”
सबसे पहले हमें मोहानी के विचारों को उनके उचित संदर्भ में स्थापित करने के लिहाज़ से डॉ बीआर आंबेडकर के एक और विचार को याद करना चाहिए। जब आंबेडकर ने 4 नवंबर, 1948 को संविधान के मसौदे को मंज़ूरी के लिए पेश किया था, तो उन्होंने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के सवाल पर संवैधानिक प्रावधान का बचाव करते हुए बात की थी। साथ ही, आंबेडकर ने कहा था कि बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों ने ग़लत रास्ते का अनुसरण किया है। उन्होंने कहा था कि बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों के वजूद को नज़रअंदाज़ तो नहीं ही कर सके, लेकिन अल्पसंख्यकों के लिए ख़ुद को अल्पसंख्यक के रूप में बनाये रखना भी ग़लत था। उन्होंने कहा, “जिस पल बहुमत अल्पसंख्यक के साथ भेदभाव बरतने की आदत छोड़ देता है, उसी पल अल्पसंख्यक रह जाने के वजूद का कोई आधार नहीं रह जाता। इस तरह की स्थिति नज़र से बाहर हो जाएगी।”
मोहानी एक बात पर आंबेडकर की बात से सहमत थे और वह बात यह थी कि उन दोनों की धारणा अल्पसंख्यकों को अल्पसंख्यक मानने की थी। साथ ही साथ संवैधानिक नज़रिये से देखें, तो ये दोनों ख़ुद ही अल्पसंख्यक समूह से आते थे। हालांकि, मोहानी ने इस बात पर ज़ोर दिया था कि अल्पसंख्यकों को अलग-अलग राजनीतिक दल इसलिए नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी राजनीतिक व्यवस्थाएँ ग़ैर-ज़रूरी होती हैं। दूसरी ओर, राष्ट्रवादी पार्टियों में शामिल होने से अल्पसंख्यकों को सत्ताधारी अभिजात वर्ग का हिस्सा बनने का मौक़ा मिलता है।
मोहानी ने देश को बहुत पहले जो सलाह दी थी, उस सलाह के उलट, आज हम कई ऐसे राजनीतिक दलों के वजूद के गवाह बने हुए हैं, जो केवल विशेष समुदायों से जुड़े मुद्दों पर अपनी आवाज़ उठाते रहते हैं। आंबेडकर ने 4 नवंबर 1948 को अपने भाषण में यह भी कहा था, “अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव नहीं बरते जाने के अपने फ़र्ज़ को महसूस करना बहुसंख्यकों का कर्तव्य है। अल्पसंख्यक बने रहेंगे या ख़त्म हो जाएंगे, यह बहुसंख्यकों के इसी अहसास पर निर्भर करता है।
आज अल्पसंख्यक पार्टियां इसीलिए मौजूद हैं, क्योंकि अल्पसंख्यक समुदायों के लोग राष्ट्रीय दलों के होने के बावजूद असुरक्षित और चिंतित महसूस कर रहे हैं। ये राष्ट्रीय दल या तो उनके हितों की नुमाइंदगी नहीं करते, या उन्हें उन पार्टियों में न्यूनतम नुमाइंदगी मिलती है, जो कि जन-केंद्रित राजनीति की नाकामी का संकेत देता है। इस तरह, हमारे पास ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन, शिरोमणि अकाली दल, बहुजन समाज पार्टी और कई दूसरी पार्टियां हैं, जो ख़ास-ख़ास समुदायों की नुमाइंदगी करने का दावा करती हैं।
हमारे पास इस समय भी ख़ास हितों के एजेंडा वाले ऐसे राजनीतिक दल हैं और कुछ जातीय या क्षेत्रीय समूहों की नुमाइंदगी करते हैं। कोई शक नहीं कि मोहानी इस तरह की राजनीतिक व्यवस्था के घोर विरोधी रहे होंगे। उनके नज़रिये से उस समय की राष्ट्रवादी पार्टियां, जो भारत के लोगों और ख़ासकर श्रमिकों और किसानों के हितों और उनकी आकांक्षाओं को समग्र रूप से व्यक्त करती थीं, एक लोकतांत्रिक देश में मौजूद होनी चाहिए। उन्होंने समय-समय पर जिन विचारों को सामने रखा था, उन विचारों को लेकर उनकी आजीवन प्रतिबद्धता बनी रही थी, और उन्होंने उन विचारों को सामने रखने को लेकर कभी भी किसी तरह का कोई संकोच नहीं किया था।
अनुवाद : रणधीर गौतम
(लेखक गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर में समाजशास्त्र के प्रोफेसर और इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसायटी के अध्यक्ष रह चुके हैं।)
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.