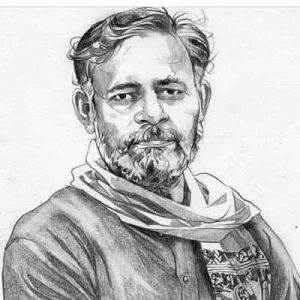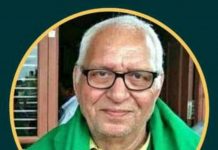— योगेन्द्र यादव —
पिछले हफ्ते जारी हुई नयी नेशनल एचीवमेंट सर्वे (एन.ए.एस.) रिपोर्ट को देखते हुए मुझे एक बैठक की याद आयी जो अब से कोई एक दशक पहले हुई थी। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (एन.सी.ई.आर.टी) ने एक बैठक में आमंत्रित किया था। इस बैठक में अगले यानी 2011 के नेशनल एचीवमेंट सर्वे की योजना बनायी जानी थी। याद आ रहा है कि मैंने वहां अपने सहकर्मियों से कहा था, “देश के स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता की बाबत आपका यह सर्वे सबसे उम्दा है और सबसे घटिया भी। सबसे उम्दा इसलिए कि आप सर्वेक्षण के लिए जो नमूना चुनते और सवाल तैयार करते हैं, वह सौ टंच खरा है और सबसे घटिया इसलिए कि कोई भी आपकी रिपोर्ट पढ़ नहीं सकता या यों कहें कि पढ़कर उसके कोई मायने-मतलब नहीं निकाल सकता।”
जैसे आत्मघात होता है वैसे ही एक शब्द शिक्षा-घात होता है। जब कोई समाज खुद अपने हाथ से आनेवाली पीढ़ियों की शैक्षिक संभावनाओं का गला दबाये तो इसे शिक्षाघात नहीं तो क्या कहें? हमलोग हाल के वक्त में शिक्षाघात के सबसे दर्दनाक मंजर के साक्षी हैं।
इसमें तो किसी शक-शुबहे की गुंजाइश ही नहीं कि शिक्षा की गुणवत्ता का मसला आज हमारी शिक्षा विषयक नीतियों का केंद्रीय मसला है। प्रासंगिक हर आयु-वर्ग के तकरीबन सभी बच्चे अब स्कूल जा रहे हैं। अब सवाल स्कूलों की पर्याप्त संख्या का नहीं रहा जो पूछा जाए कि इतने स्कूल है ही कहां कि सभी बच्चों का दाखिला हो। लेकिन जहां तक शिक्षकों की संख्या का सवाल है—वह एक गंभीर बाधा के रूप में कायम है। मतलब, असल मुद्दा अब स्कूलों की संख्या में कमी या स्कूलों में बच्चों के दाखिले का नहीं बल्कि अब असल मुद्दा ये है कि क्या बच्चे स्कूलों में जाकर कुछ सीख पा रहे हैं और क्या उन्हें किन्हीं मजबूरियों के कारण स्कूल छोड़ना नहीं पड़ रहा? (स्कूली पढ़ाई के बीच में ही छूट जाने की इस क्रूर घटना को सरकारी भाषा में ड्रॉप-आउट कहा जाता है)
सीखवन का मापन बड़ा कठिन काम है
जाहिर है, फिर सवाल ये बनेगा कि बच्चे अगर स्कूलों में कुछ सीख पा रहे हैं तो उस सीखे हुए का मापन कैसे हो, कैसे जानें कि क्या सीखा और कितना सीखा? शिक्षा से संबंधित मामलों के कुछ विशेषज्ञ सीखवन के मापन जैसे विचार का ही विरोध करते हैं (और ऐसे विशेषज्ञों में प्रोफेसर कृष्ण कुमार भी शामिल हैं जिनकी राय का मैं इन मामलों में सबसे ज्यादा सम्मान करता हूं)। उनका तर्क यह है कि जितनी और जैसी भी जांच कर लो, बच्चे ने क्या सीखा और कितना सीखा, इसे ठीक-ठीक मापा नहीं जा सकता क्योंकि सीखना हमेशा एक बहु-आयामी प्रक्रिया है। इन विशेषज्ञों की यह बात जितनी ठीक है उतनी ही ठीक ये बात भी है कि बच्चों के माता-पिता और साथ ही नीति-निर्माताओं के हाथ में भी कोई पैमाना होना जरूरी है (चाहे वह अनगढ़ ही क्यों ना हो) जिसके सहारे वे शिक्षण की गुणवत्ता का आकलन कर सकें। इस जरूरत की पूर्ति नेशनल एचीवमेंट सर्वे (एन.ए.एस) कर सकता है लेकिन अभी तक कर नहीं सका है।
बीते 16 सालों से ‘एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट’ (असर) ने इस जरूरत की पूर्ति की है। ‘प्रथम’ नाम की स्वयंसेवी संस्था के सर्वेक्षक बहुत से ग्रामीण घरों में जाते हैं और वहां बच्चों से भाषाई तथा गणितीय योग्यता के आकलन से संबंधित कुछ बुनियादी सवाल पूछते हैं। यह सर्वेक्षण बहुत बड़े पैमाने पर होता है और हमारे सामने एक सीधी-सरल मगर बड़ी स्पष्ट तस्वीर पेश करता है कि ग्रामीण स्कूलों में सीखवन की दशा कितनी गयी-बीती है। ‘असर’ ने अपने निष्कर्षों से देश को चौंकाया है और साल-दर-साल ‘असर’ के निष्कर्ष कमोबेश एक-से रहे हैं। ‘असर’ ने हमें बताया है कि पांचवीं क्लास के आधे से ज्यादा बच्चे अपनी भाषा में दूसरी कक्षा के लिए बनी पुस्तक का पूरा एक अनुच्छेद भी पढ़ पाने में समर्थ नहीं। यह एक बनी-बनायी और अनगढ़ जान पड़ती कसौटी है जो शायद उन पद्धतिगत (मेथडोलॉजिकल) उच्च मानकों पर सौ टंच खरा ना उतरे जिनके पालन की किसी सर्वेक्षण आधारित शोध से अपेक्षा रखी जाती है। ‘असर’ के आधार पर अलग-अलग समय में क्या शैक्षिक परिलब्धियां रहीं इसकी तुलना करना कठिन है।
नेशनल एचीवमेंट सर्वे (एन.ए.एस.) इसका एक विकल्प मुहैया कराता है। यह सर्वेक्षण अपने विस्तार और गहराई में सचमुच प्रभावशाली है। इस सर्वेक्षण में तीसरी, पांचवीं, आठवीं तथा दसवीं क्लास के विद्यार्थियों की तमाम बुनियादी विषयों की जानकारी का टेस्ट लिया जाता है। जांच-परख के प्रश्न और तौर-तरीके बड़ी बारीकी से तैयार किये जाते हैं। सर्वेक्षण में लिया गया नमूना तो और भी गजब है। मिसाल के लिए, हाल के एन.ए.एस. सर्वेक्षण को ले सकते हैं जो साल 2021 के नवंबर में हुआ। इसमें 1.18 लाख स्कूलों को नमूने के तौर पर लिया गया जिसमें दो तिहाई ग्रामीण इलाकों के हैं और नमूने के तौर पर चुने गये विद्यालयों में सरकारी स्कूलों के साथ-साथ सहायता-प्राप्त (एडेड) स्कूल तथा निजी श्रेणी के भी स्कूल शामिल हैं। विभिन्न कक्षाओं में पढ़नेवाले लगभग 34 लाख विद्यार्थियों की जांच की गयी। इस नाते हम संकलित आंकड़ों को जिलावार और राज्यवार श्रेणीक्रम में सजाकर देख-परख सकते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (एन.सी.ई.आर.टी.) तथा शिक्षा-जगत के प्रशासक अपनी पीठ थपथपा सकते हैं कि उन्होंने शायद शिक्षा की गुणवत्ता के आकलन से संबंधित दुनिया का सबसे बड़ा सर्वेक्षण कर दिखाया है। मुझे ये देखकर खुशी हुई कि सर्वेक्षण की रिपोर्टिंग और प्रस्तुति में भी सुधार आया है।
लेकिन एक गंभीर मसला बना हुआ है। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट (असर) के विपरीत नेशनल एचीवमेंट सर्वे (एन.ए.एस.) हमेशा स्कूली परिसर में ही किया जाता है। सो, ऐसे में इस बात से इनकार करना मुश्किल है कि कुछ कर दिखाने को आतुर अधिकारी और चिन्ता में पड़े शिक्षक विद्यार्थियों की परीक्षा हॉल में ‘मदद‘ करते होंगे ताकि नतीजे बेहतर आएं। इस नाते, विद्यार्थियों की शैक्षिक परिलब्धि की राज्यवार तुलना के काम से बाज आना बेहतर होगा भले ही ऐसी तुलना की मीडिया में बड़ी-बड़ी सुर्खियां बनती हों। लेकिन, जहां तक दो समयावधियों के बीच और वर्गों तथा सामाजिक समूहों के बीच तुलना की बात है, नेशनल एचीवमेंट सर्वे एक बेशकीमती पैमाना साबित हो सकता है।
देश की स्कूली शिक्षा के बारे में एन.ए.एस. क्या बताता है
नये एन.ए.एस. सर्वे के तथ्यों से मुख्य रूप से चार संदेश निकलते हैं। तीन संदेश तो बा-आसानी पढ़े जा सकते हैं लेकिन चौथा संदेश आंकड़ों की तहों के भीतर बड़े जतन से छिपाया हुआ है।
पहला संदेश ये निकलता है कि स्कूली शिक्षा गुणवत्ता के हिसाब से खराब है। अगर व्यापक रूप से देखें यानी सभी कक्षाओं को ध्यान में रखते हुए कहें तो मातृभाषा को छोड़कर लगभग हर विषय में छात्रों को हासिल अंक 60 प्रतिशत से कम है ( पर्यावरण विज्ञान में 59, अंग्रेजी में 55, गणित में 53, समाज विज्ञान में 49 और प्राकृतिक विज्ञान में 46)। हां, नेशनल एचीवमेंट सर्वे से निकलती यह तस्वीर एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट (असर) से निकलती तस्वीर से कुछ बेहतर जरूर है। लेकिन हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि एन.ए.एस. में शहरी तथा प्राइवेट स्कूलों को भी शामिल किया गया है और यह सरल किस्म की जांच-परख विभिन्न परिस्थितियों में स्कूली परिसर के अंदर ही सम्पन्न हुई है।
दूसरा संदेश ये कि जांच-परख के काम में जैसे-जैसे हम ऊंची कक्षाओं की तरफ बढ़ते हैं, नजर आता है कि छात्रों की शैक्षिक परिलब्धि घटती जा रही है। मिसाल के लिए, तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों को भाषा में 65 प्रतिशत अंक हासिल हैं लेकिन पांचवीं क्लास के विद्यार्थियों के बीच भाषाई योग्यता के मामले में हासिल अंक घटकर 62 प्रतिशत पर चले आते हैं। इसी तरह आठवीं क्लास के विद्यार्थियों को भाषाई योग्यता के मामले में हासिल अंक 60 प्रतिशत है तो दसवीं क्लास के विद्यार्थियों को महज 52 प्रतिशत। अंकों की ऐसी ही घटत हम गणित तथा कमोबेश अन्य विषयों में पाते हैं। जब तक परीक्षण का तरीका बदल नहीं जाता इस निष्कर्ष को नकारना मुश्किल है कि कोई छात्र स्कूली शिक्षा में जितने ज्यादा साल गुजारता है, उसकी शैक्षिक परिलब्धि में उतनी ही कमी आती जाती है। यह बात हमारी शिक्षा-व्यवस्था पर लगे एक गहरे दाग की तरह है।
सर्वेक्षण से निकलता तीसरा संदेश और भी ज्यादा बुरा है। छात्रों की स्कूली शिक्षा के साल जितने ज्यादा बढ़ते हैं, सामाजिक वर्गों के लिहाज से छात्रों की शैक्षिक परिलब्धि में उतना ही ज्यादा अंतर आता जाता है।
मिसाल के लिए, सरकारी और प्राइवेट स्कूल में तीसरी कक्षा में पढ़नेवाले छात्रों की शैक्षिक परिलब्धि में शायद ही कोई अन्तर है। लेकिन पांचवीं क्लास तक आते-आते प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में पढ़नेवाले बच्चों के बीच पांच प्रतिशत का अन्तर दीख पड़ेगा आपको, प्राइवेट स्कूल सरकारी स्कूलों पर पांच प्रतिशत की बढ़त बनाते नजर आएंगे। दसवीं कक्षा के विद्यार्थियों के बीच (प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में) यह अन्तर और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है। तुलना करने पर यही बात सामान्य कोटि के छात्रों तथा अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों के बीच नजर आएगी आपको। दीख पड़ेगा कि तीसरी क्लास तक तो विभिन्न सामाजिक वर्ग के छात्रों की शैक्षिक परिलब्धि में अन्तर ना के बराबर है लेकिन ये ही छात्र जब दसवीं क्लास तक पहुंचते हैं तो उनकी शैक्षिक परिलब्धि में बड़ा अन्तर आ जाता है।
गैर-बराबरी से भरे किसी समाज में शिक्षा का मकसद पहले से चली आ रही नुकसानदेह परिस्थितियों में कमी लाने का होना चाहिए। लेकिन, जान पड़ता है कि हमारी शिक्षा-व्यवस्था ठीक इसके उलट कर रही है। हमारे देश में शिक्षा पहले से चली आ रहे विशेषाधिकारों को हस्तांतरित करने और उत्तरोत्तर आगे बढ़ाते जाने का प्रभावी-तंत्र है।
शिक्षा पर महामारी का असर बताते आंकड़े
सर्वेक्षण से निकलता चौथा संदेश सबसे अहम है लेकिन इस संदेश को एन.ए.एस. की रिपोर्ट में बड़े जतन से छिपा दिया गया है। कोरोनाबंदी के दौरान लंबे समय तक स्कूलों के बंद रहने के बाद शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर हुआ यह अखिल भारतीय स्तर का पहला सर्वेक्षण था। जाहिर है, फिर कोई भी व्यक्ति पूछना चाहेगा कि आखिर स्कूलों के बंद रहने से शिक्षा की गुणवत्ता पर क्या और कैसी चोट पड़ी? एन.ए.एस. की रिपोर्ट में इस सवाल का जवाब बतानेवाले आंकड़े शामिल नहीं हैं। मुझे लगता है, निर्देश दिया गया होगा कि ऐसे आंकड़ों को रिपोर्ट में शामिल नहीं करना है। शुक्रिया कहना बनता है ‘द हिन्दू’ के ‘डेटा प्वाइंट टीम’ का, जो उसने साल 2017-18 की एन.ए.एस. की रिपोर्ट के तथ्यों को खॅंगाला और विभिन्न कक्षाओं तथा विषयों के अंक आमने-सामने रखकर उनकी इस बार की रिपोर्ट के तथ्यों से सावधानीपूर्वक तुलना की।
इस तुलना से निकलते नतीजे दिल को चोट पहुंचाने वाले हैं। कोरोनाबंदी के दौरान छात्रों की शैक्षिक परिलब्धि में भारी गिरावट आयी है। तीसरी क्लास के छात्रों की शैक्षिक परिलब्धि में यह गिरावट 3 प्रतिशत अंकों (सभी विषयों के लिए) की है तो दसवीं कक्षा के छात्रों के लिए गणित विषय में 7 प्रतिशत की और विज्ञान के विषय में 9 प्रतिशत की गिरावट आयी है। विभिन्न सामाजिक वर्गों के छात्रों की शैक्षिक परिलब्धि के लिहाज से भी यही बात कही जा सकती है। ग्रामीण इलाके के स्कूली बच्चों की शैक्षिक परिलब्धियों में गिरावट शहरी इलाके के स्कूली बच्चों की तुलना में कहीं ज्यादा है। हालांकि लैंगिक आधार पर देखें तो छात्र-छात्राओं की शैक्षिक परिलब्धियों के बीच कोरोनाबंदी से पहले और कोरोनाबंदी के बाद के वक्त में अन्तर बहुत मामूली सा है लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्रों की शैक्षिक परिलब्धियों में तुलनात्मक रूप से कहीं ज्यादा गिरावट आयी है।
महामारी और कोरोनाबंदी के कारण शिक्षा के क्षेत्र में हुए नुकसान का आकलन करने के लिए वैश्विक स्तर पर जो अनुसंधान हुए हैं उनके निष्कर्षों से एन.ए.एस. सर्वेक्षण के नतीजे मेल खाते हैं। जैसा कि मैंने अपने पहले के एक लेख में कहा है—भारत महामारी और कोरोनाबंदी से सबसे ज्यादा नुकसान उठानेवाले देशों में एक बनकर सामने आया है। एन.ए.एस. के आंकड़े बता रहे हैं कि हमारी आँखों के सामने करोड़ों छात्रों के करिअर और सपनों की कब्र खुद रही है।
(द प्रिंट से साभार)