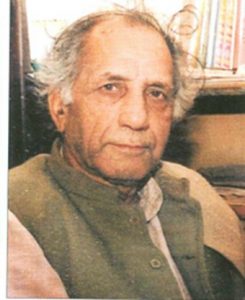
— मस्तराम कपूर —
नेताजी सुभाषचंद्र बोस को भारत की स्वाधीनता के आंदोलन की क्रांतिकारी धारा का शलाका पुरुष कहा जा सकता है। इस वक्तव्य का अर्थ अन्य क्रांतिकारियों को उनकी तुलना में कम बताना नहीं है। इसका अर्थ है कि स्वाधीनता का क्रांतिकारी आंदोलन सुभाष के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज के रूप में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँचा। क्रांतिकारी आंदोलन का प्रारंभ वैयक्तिक प्रयासों के रूप हुआ। बंगाल-विभाजन से प्रेरित क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण मुख्य रूप से व्यक्तिगत आतंकवाद तक सीमित रहा। गदर पार्टी ने सेनाओं में विद्रोह कराने के जो प्रयास किए उनमें आंदोलन को सामूहिक रूप मिलता दिखाई दिया किंतु वह क्षणिक ही रहा और स्थायी प्रभाव नहीं बन सका। चंद्रशेखर आजाद, भगतसिंह और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के अन्य साथियों द्वारा चलाया गया क्रांतिकारी आंदोलन स्पष्ट विचारधारा और मजबूत संगठन तो बना पाया किंतु उनकी रणनीति व्यक्तिगत आतंकवाद से आगे नहीं बढ़ सकी।
केवल सुभाषचंद्र बोस के नेतृत्व में चले क्रांतिकारी आंदोलन को संपूर्ण वैचारिक और संगठनात्मक आधार मिला और उसने विदेशी सत्ता के खिलाफ सशस्त्र युद्ध का रास्ता चुना।
यह प्रयास सफल नहीं हुआ किंतु इसे असफल भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसने स्वतंत्रता की नींव रखी और विदेशी सत्ता को बोध करा दिया कि उसका इस देश में टिके रहना अब संभव नहीं है। आजाद हिंद फौज और ‘भारत छोड़ो’ का भूमिगत विद्रोह इस बात का स्पष्ट संकेत था कि भारत की जनता अब गुलामी को बर्दाश्त नहीं करेगी और विदेश सत्ता के लिए देश छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है।
सुभाषचंद्र बोस का पुनर्मूल्यांकन करते हुए समाजवादी चिंतक मधु लिमये ने अपनी पुस्तक प्राइम मूवर्स में लिखा : “आने वाली पीढ़ियाँ सुभाष को उनके प्रयास की सफलता के लिए नहीं, उस प्रयास की प्रतिबद्धता के लिए याद रखेंगी। देशवासियों के हृदय में उनके लिए स्थायी स्थान होगा, इसलिए नहीं कि उन्होंने क्या हासिल किया बल्कि इसलिए कि उन्होंने क्या करना चाहा और उसके लिए कितना साहस दिखाया।’’
गांधीजी ने अपने एक पत्र में (गुरुदेव रवींद्र को लिए लिखे गए) सुभाष को अपना गुमराह पुत्र लिखा था। यह इसलिए कि सुभाष को गांधीजी के अहिंसा के सिद्धांत पर पूरी आस्था नहीं थी। सुभाष के मन में भी गांधीजी के प्रति असीम आदर भाव था बावजूद कतिपय मतभेदों के। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का संबोधन उन्होंने ही दिया था। इसमें कोई संदेह नहीं कि वे गांधीजी से अधिक बंगाल के प्रमुख नेता देशबंधु चित्तरंजन दास के राजनीतिक विचारों से प्रभावित थे। गांधीजी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर जब चित्तरंजन दास ने अपनी बढ़िया वकालत छोड़ दी तो सुभाषचंद्र बोस ने भी आईसीएस की डिग्री छोड़ दी।

आईसीएस को उस समय बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाता था। मोतीलाल नेहरू के मन में बड़ी साध थी कि उनका बेटा (जवाहरलाल) आईसीएस बने। सुभाष ने न केवल इसे पास किया बल्कि उत्तीर्ण विद्यार्थियों में चौथे स्थान पर रहे। किंतु उन्होंने इस उपलब्धि को भारत माता की सेवा की तुलना में तिरस्कार से देखा। संभवतः इसका कारण उनका आध्यात्मिक रुझान भी था जिसके कारण भोगवादी जीवन के प्रति उनमें अरुचि थी। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानन्द और अरविंद के गहरे प्रभाव के साथ-साथ उनपर हीगेल का भी गहरा प्रभाव था जिन्होंने राज्य को ब्रह्म जैसी निरपेक्ष सत्ता के रूप में प्रस्तुत किया।
कांग्रेस में सुभाष और जवाहरलाल नेहरू युवा पीढ़ी के नेता थे। दोनों में जोश था और गांधीजी से उनके मतभेद समय-समय पर उभरते रहते थे। इसका कारण दो पीढ़ियों का अंतर तो था ही किंतु मुख्य था शिक्षा-दीक्षा का प्रभाव।
सुभाष और जवाहरलाल पश्चिमी शिक्षा की निर्मिति थे। जवाहरलाल पर मार्क्स का और सुभाष पर हीगेल का प्रभाव अधिक था। गांधीजी पश्चिमी शिक्षा और पश्चिमी सभ्यता को संदेह की नजर से देखते थे और वे एक ऐसा रास्ता अपनाकर चल रहे थे जो नितांत नया था और जिसे समझ पाना सुभाष और जवाहरलाल दोनों के लिए कठिन था। इन दोनों की तुलना में डॉ. राममनोहर लोहिया, गांधी को समझने में सफल रहे क्योंकि लोहिया खुद भी पश्चिमी विचारधाराओं और पश्चिमी सभ्यता के आलोचक थे। गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत और साध्य-साधन समन्वय के सिद्धांत को समझ पाना सुभाष-नेहरू दोनों के लिए आसान नहीं था।
सुभाष जब आईसीएस कर लंदन से लौटे तो बंबई में गांधीजी से मिलने गए। उनकी यह पहली मुलाकात सुभाष के लिए निराशाजनक रही। तब गांधीजी ने उन्हें चित्तरंजन दास से मिलने की सलाह दी। चौरी-चौरा की घटना के बाद गांधीजी ने जब असहयोग आंदोलन अचानक वापस ले लिया तो उस समय के अन्य नेताओं की तरह सुभाष को भी बहुत निराशा हुई। वास्तव में इस निराशा का कारण था कि चित्तरंजन दास, मदनमोहन मालवीय, एम.आर. जयकर आदि नेताओं को लगता था कि ब्रिटिश सरकार चेम्सफोर्ड सुधारों के अंतर्गत भारत को प्रांतीय स्वायत्तता तथा केंद्रीय सत्ता में कुछ साझेदारी देने वाली थी और गांधी की कार्रवाई ने इसमें विघ्न डाल दिया था। चित्तरंजन दास को यह बोध बहुत अधिक था और सुभाष भी उससे प्रभावित हुए। हालांकि आगे चलकर सुभाष ने अंग्रेजों के साथ किसी भी तरह का सहयोग या समझौता करने के प्रति घोर अरुचि दिखाई, पर बीस के दशक के उन वर्षों में वे सहयोगवादियों के साथ रहे। तथापि गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन के दौरान एक शक्तिशाली और जीवंत पार्टी का रूप लिया इसकी सुभाष ने दिल खोलकर प्रशंसा की।
सुभाष को संसदीय राजनीति से विशेष प्यार नहीं था, आगे भी नहीं रहा, तथापि उस समय वे संसदीय राजनीति के लिए उत्सुक स्वराजवादियों की ओर झुके रहे। इसके विपरीत जवाहरलाल नेहरू ने अपने को स्वराज पार्टी की गतिविधियों से अलग रखा। सुभाष की तुलना में नेहरू की गांधी जी से अधिक निकटता जो आगे चलकर देखने को मिली उसका एक कारण यह भी रहा होगा। सुभाष ने स्वराज पार्टी को गांधी की ‘तर्कहीन नीति’ के विपरीत ‘तर्कसिद्ध विद्रोह’ कहा। वास्तव में गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम युवा पीढ़ी के लिए उबाऊ थे, उनमें कोई एडवेंचर नहीं दीखता था। सरदार पटेल और नेहरू ने किसान-मजदूर आंदोलनों में एडवेंचर की तलाश की।

असहयोग आंदोलन की वापसी के बाद बंगाल में चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी को मजबूत करने के लिए क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े हुए लोगों को बड़ी संख्या में कांग्रेस में लाना शुरू किया। चित्तरंजन दास के निधन (1925) के बाद उत्तरदायित्व मुख्य रूप से सुभाष ने संभाला। उनके ‘जुगांतर’ ग्रुप के साथ घनिष्ठ संबंध थे। उनके प्रतिद्वंद्वी जे.एम. सेनगुप्ता थे जिनकी सहानुभूति अनुशीलन समिति से थी। इन क्रांतिकारियों का बंगाल के भद्रलोक वर्ग पर इतना प्रभाव था कि कोई भी नेता इसके साथ संबंध होने के आरोप से नहीं बच सकता था (केवल गांधीवादी सतीशचंद्र दासगुप्ता इसके अपवाद थे) अतः जैसे तिलक क्रांतिकारियों के साथ संबंधों की वजह से अंग्रेजों की नजर में संदिग्ध रहे उसी प्रकार सुभाष के बारे में भी अंग्रेजों को यह शुबहा रहा कि उनके क्रांतिकारी ग्रुपों के साथ घनिष्ठ संबंध थे। किंतु वे इस बात को कभी सिद्ध नहीं कर सके। इसी संदेह के कारण बीस के दशक के मध्य में ब्रिटिश सरकार ने सुभाष को बर्मा (म्यांमार) की मांडले जेल में नजरबंद रखा जहां किसी समय तिलक को भी रखा गया। सन् 1932 में भी उन्हें इस संदेह पर पकड़ा गया कि वे बंगाल के क्रांतिकारियों को मदद देते हैं। बाद में उन्हें उपचार के लिए विदेश जाने की अनुमति दे दी किंतु उनके लौटने पर पाबंदी लगाए रखी।
कांग्रेस के 1928 के कलकत्ता अधिवेशन में सुभाष, जवाहरलाल और उनके युवा साथियों ने पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव रखा। गांधी ने युवा नेताओं की भावनाओं को समुचित स्थान देते हुए यह मान लिया कि एक साल में यदि हमें ‘डोमीनियन स्टेटस’ नहीं मिलता तो हम कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वाधीनता घोषित कर देंगे। सुभाष इससे सहमत हो गए किंतु बंगाल के प्रतिनिधियों द्वारा घेराव किए जाने के बाद मत-विभाजन कराने के लिए तैयार हो गए। उनका प्रस्ताव गिर गया। गांधीजी को युवा नेताओं की यह बात पसंद नहीं आई कि एक बार किसी बात पर सहमत होने के बाद वे तुरंत अपने विचार बदल लेते हैं। उन्होंने इस ढुलमुलपन को नेतृत्व की कमजोरी बताया।
अगले वर्ष 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ जहां जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पास हुआ। सुभाष को इस बात पर नाराजगी हुई कि गांधी ने कांग्रेस को वामपक्ष के एक तेजस्वी नेता (जवाहरलाल) को, डमी अध्यक्ष बनाकर फोड़ लिया। कांग्रेस की नई कार्यसमिति में सुभाष और श्रीनिवास आयंगार को स्थान नहीं मिला। इससे भी सुभाष को निराशा हुई और उन्होंने कहा कि गांधी ‘आज्ञाकारी कार्यसमिति’ चाहते थे। उन्होंने नई पार्टी बनाने की घोषणा की किंतु सविनय अवज्ञा आंदोलन के तूफान में योजना धरी की धरी रह गई।
1934 में कांग्रेस के भीतर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। सुभाष और जवाहरलाल इस ग्रुप के स्वाभाविक नेता माने गए यद्यपि उन्होंने कभी इसकी सदस्यता ग्रहण नहीं की। कांग्रेस के भीतर इस वामपंथी ग्रुप को (जिसमें कई कम्युनिस्ट भी शामिल हुए) सुभाष-नेहरू का ही ग्रुप माना जाने लगा।
उन्हीं दिनों गांधी ने समाजवादियों से अपने मतभेद प्रकट किए। उन्होंने कहा कि समाजवादियों की अहिंसा के सिद्धांत पर पूरी आस्था नहीं है और वे अहिंसा को केवल रणनीति मानते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी कांग्रेस में मेरे जैसे आदमी के लिए जगह नहीं होगी और उन्होंने चवन्नी सदस्यता भी छोड़ दी।

दरअसल गांधीजी समाजवादियों से इसलिए भी खफा थे क्योंकि उन्होंने पूना समझौते के बाद उनके हरिजन सेवक संघ और अस्पृश्यता उन्मूलन कार्यक्रमों का या तो विरोध किया था या उनके प्रति उदासीनता दिखाई थी। जवाहरलाल और सुभाष दोनों ने गांधी के इन कार्यक्रमों को संघर्ष से पलायन माना था। गांधीजी द्वारा समाजवादियों की आलोचना मुख्य रूप से अपने दो शिष्यों- जवाहरलाल और सुभाष- के रवैये के कारण थी। इसके बाद सुभाष तो उनसे दूर ही होते गए लेकिन जवाहरलाल दूर होने के तेवर दिखाते हुए पुनः गांधी की ओर लौटते रहे।
कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन (1939) के समय गांधी और सुभाष के मतभेद चरम बिंदु पर पहुंच गए जब नेहरू से प्रेरित होकर समाजवादियों ने पंत-प्रस्ताव का समर्थन किया। इसमें कहा गया था कि सुभाष जो पुनः कांग्रेस-अध्यक्ष चुने गए थे, गांधीजी के परामर्श से अपनी कार्यसमिति बनाएं। सुभाष ने कांग्रेस छोड़कर फारवर्ड ब्लाक पार्टी बना ली। जवाहरलाल ने अपने गुरु से असहमत रहते हुए उनसे संबंध नहीं तोड़ा जबकि सुभाष ने संबंध तोड़ने में भी हिचक नहीं दिखाई।
जवाहरलाल और सुभाष के विचारों में एक विशेष अंतर भी था। जवाहरलाल कहते थे कि फासीवाद और साम्यवाद में किसी एक को चुनना पड़े तो वे साम्यवाद को चुनेंगे। सुभाष इससे असहमत थे। वे साम्यवाद को भी पसंद नहीं करते थे (उसकी नितांत भौतिकता के कारण) और यह मानते थे कि फासीवाद तथा साम्यवाद के संश्लेषण से एक नई व्यवस्था बन सकती है। उन्हें फासीवाद और साम्यवाद दोनों ही नापसंद थे किंतु इनके प्रति एलर्जी जैसी भावना नहीं थी जबकि नेहरू में फासीवाद के प्रति एलर्जी थी। इसलिए आगे चलकर सुभाष ने भारत की स्वतंत्रता के लिए दुश्मन के दुश्मन को दोस्त मानने की नीति के अनुसार जर्मनी, इटली और जापान जैसी फासीवादी ताकतों से मदद लेने में हिचक नहीं दिखाई जबकि जवाहरलाल नेहरू को यह बात बहुत अरुचिकर लगी। कम्युनिस्टों ने तो सुभाष को फासीवादी ही बना दिया।
राजनीति के प्रति जवाहरलाल की दृष्टि कवि की तरह भावनात्मक अधिक थी जबकि सुभाष व्यवहारवादी थे। यह बात 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडलों के निर्माण के समय भी सामने आती है।
जवाहरलाल ने मुस्लिम लीग के साथ संयुक्त मंत्रिमंडल बनाने के प्रस्ताव का विरोध किया जबकि सुभाष ने आसाम में संयुक्त मंत्रिमंडल बनवाया और बंगाल में भी इसकी कोशिश की किंतु बिड़ला और मौलाना अबुल कलाम आजाद के आग्रह के कारण वे इसमें सफल नहीं हुए। गांधीजी ने भी माना कि आसाम के कांग्रेसी नेताओं ने मंत्रिमंडल के त्यागपत्र के मामले में सुभाष के बजाय मौलाना की सलाह मानकर गलती की (आसाम मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र नहीं दिया था) उधर संयुक्त प्रांत में संयुक्त सरकार न बनाने की जिद के कारण जिन्ना बेहद रुष्ट हो गए और पृथक देश की मांग की ओर झुक गए। देश के विभाजन के बीज यहीं पड़े।
गांधी से अपने तमाम मतभेदों के बावजूद सुभाष का मन उस समय गांधी के प्रति प्रशंसा-भाव से भर उठा जब उनका ‘भारत छोड़ो’ प्रस्ताव सामने आया। ब्रिटिश सरकार ने इसका मसौदा ए.आई.सी.सी. के दफ्तर पर छापा मारकर पकड़ लिया था और उसे प्रकाशित कर दिया था।
बंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में 8 अगस्त, 1942 को गांधीजी ने जब ‘करो या मरो’ का आह्वान किया तो सुभाष ने गदगद होकर लिखा :
“इसमें कोई संदेह नहीं कि कांग्रेस का प्रस्ताव भारत की विशाल जनता की इच्छा के निकटतम है। इसके साथ कांग्रेस उस विचार के निकट आ गई है जिसे यह लेखक हमेशा व्यक्त करता रहा है अर्थात भारत की समस्याओं के समाधान के लिए भारत में ब्रिटिश सत्ता का विनाश पहली शर्त है और भारत की जनता को यह लक्ष्य प्राप्त करने के लिए युद्ध करना पड़ेगा।”
सुभाषचंद्र बोस जिस प्रकार 1941 में भेष बदलकर ब्रिटिश पुलिस को चकमा देते हुए पेशावर, काबुल, मास्को और फिर बर्लिन पहुंचे यह एक सनसनीखेज कहानी है और इसने न सिर्फ सारे भारतवासियों के मन में उत्साह जगाया, गांधी और मौलाना को भी भाव-विभोर कर दिया। बर्लिन से सिंगापुर पहुंचकर उन्होंने आजाद हिंद फौज की कमान संभाली और भारत की मुक्ति के लिए दिल्ली की ओर बढ़ने लगे। उत्तर-पूर्वी सीमा प्रदेशों में पहुंचने के बाद उनका अभियान रुक गया क्योंकि जापान ने हिरोशिमा तथा नागासाकी पर परमाणु बम गिराए जाने के बाद आत्मसमर्पण कर दिया। कुछ दिन बाद सुभाषचंद्र बोस का भी विमान दुर्घटना में निधन हो गया।
सुभाषचंद्र बोस ने अपने अदम्य कारनामों से भारत की जनता में जो आत्मविश्वास भरा उसने स्वाधीनता आंदोलन को परिणति तक पहुंचाने में मदद की। बच्चे-बच्चे के मुंह पर सुभाष का नाम और ‘जयहिंद’ का नारा चढ़ गया। इतिहासकारों में उनकी नीतियों को लेकर बहस चलती रही और आगे भी चलेगी लेकिन समय ने उन नीतियों की सार्थकता सिद्ध कर दी।
दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान जवाहरलाल जैसे नेता भी विदेशों से मदद लेने की बात सोचने लगे। वे इसके लिए चीन, अमरीका और इंग्लैंड की लेबर पार्टी की ओर देखते थे। सुभाष ने शत्रु के शत्रु को दोस्त बनाकर कर अपना लक्ष्य सिद्ध करना चाहा जो अधिक व्यावहारिक था। गांधीजी को भी सुभाष की दृष्टि अपनानी पड़ी। स्वाधीनता आदमी का अस्तित्व है, यह उसका जीवन ही है। जब इसकी रक्षा का प्रश्न सामने होता है तो हिंसा अहिंसा का व्यामोह नहीं रहता। आदमी को हर साधन से अपनी आजादी की और अपने जीवन की रक्षा करनी होती है। महात्मा गांधी ने ‘करो या मरो’ के अपने संदेश में यह बात स्वीकार की। देश के विभाजन के फलस्वरूप हुए सांप्रदायिक दंगों के संदर्भ में भी उन्हें यह बात कहनी पड़ी।
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

















